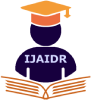
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
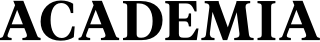













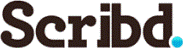




सिरोही के पुरातात्विक स्थलः चन्द्रावती के विशेष संदर्भ में
| Author(s) | SOHAN LAL |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की विविध सभ्यताओं, धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक संरचनाओं को अपने भीतर समाहित किया है। यह प्रदेश न केवल वीरता, स्थापत्य और स्थापत्य की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी धरती अनेक सभ्यताओं की जन्मस्थली और गवाह भी रही है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में फैली पुरातात्विक संपदा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की भूमि पर आदिकाल से ही मानव सभ्यता का विकास होता रहा है। इन्हीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है सिरोही ज़िला, जो अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। सिरोही न केवल प्राकृतिक दृष्टि से सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि इसका भौगोलिक स्थान भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। सिरोही ज़िले में कई ऐतिहासिक नगर और पुरातात्विक स्थल स्थित हैं, जिनमें से चन्द्रावती का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। चन्द्रावती एक प्राचीन नगर रहा है जिसका आरंभिक विकास संभवतः मौर्य काल में हुआ और आगे चलकर यह गुर्जर-प्रतिहार, परमार तथा सोलंकी शासकों के अधीन एक समृद्ध नगर के रूप में उभरा। यह नगर बाणास नदी के तट पर स्थित था और अपने समय में व्यापार, धर्म, संस्कृति, और स्थापत्य के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता था। चन्द्रावती की ऐतिहासिकता का उल्लेख कई विदेशी यात्रियों, राजवंशीय अभिलेखों और पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजों में मिलता है। यहाँ मिले मंदिरों के अवशेष, मूर्तियाँ, तोरण, स्तंभ तथा जल संरचनाएँ यह दर्शाती हैं कि यह नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि नगर नियोजन और स्थापत्य में भी अग्रणी था। वर्तमान में चन्द्रावती के अवशेष खंडहरों के रूप में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें छिपी हुई कला, संस्कृति और सभ्यता की कहानियाँ आज भी पुरातत्व और इतिहास के शोधकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। यह स्थल पुरातात्विक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, उज्जैन या किसी अन्य प्राचीन नगर के अवशेष। दुर्भाग्यवश यह स्थल आज पर्याप्त शोध, संरक्षण और प्रचार से वंचित रहा है। यह शोध पत्र सिरोही ज़िले की पुरातात्विक संपदा के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिसमें चन्द्रावती पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। शोध का उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को उजागर करना है, बल्कि यह भी देखना है कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसमें कौन-कौन सी प्रमुख संरचनाएँ पाई जाती हैं, उनका स्थापत्य और मूर्तिकला से क्या संबंध है, और इस क्षेत्र में पर्यटन तथा संरक्षण की क्या संभावनाएँ मौजूद हैं। चन्द्रावती की ऐतिहासिकता के विश्लेषण के साथ-साथ यह शोध यह भी रेखांकित करने का प्रयास करता है कि कैसे ऐसे स्थल आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पर्यटन विकास का माध्यम बन सकते हैं। साथ ही, यह शोध उन चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है जो इन पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन में बाधा बन रही हैं। अतः यह प्रस्तावना केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि एक आह्वान है कि हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनना होगा ताकि हमारी भावी पीढ़ियाँ भी इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें। 2. शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य राजस्थान अपने ऐतिहासिक गौरव, समृद्ध स्थापत्य और पुरातात्विक वैभव के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध रहा है। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, नागौर और जोधपुर जैसे नगरों में पुरातत्व विषयक अनेक शोध और उत्खनन कार्य किए गए हैं, जिससे वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को पहचान, संरक्षण और पर्यटन के अवसर प्राप्त हुए हैं। परंतु राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित सिरोही ज़िला, विशेषकर चन्द्रावती जैसा प्राचीन नगर, अभी भी व्यापक शोध और संरक्षण के प्रयासों से वंचित है। चन्द्रावती का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गूढ़ है। यह नगर न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध रहा, बल्कि इसकी नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणाली भी अपने समय में अत्याधुनिक मानी जाती थी। यहां की वास्तुशिल्प और मूर्तिकला में परमार और सोलंकी शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त, चन्द्रावती का विनाशकाल और उसके कारणों को समझना भी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करता है। इन सबके बावजूद, चन्द्रावती जैसे नगर को न तो भारतीय इतिहास की मुख्यधारा में समुचित स्थान मिला है, न ही इसकी पुरातात्विक महत्ता को पर्याप्त प्रचार और संरक्षण मिल सका है। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय उपेक्षा, प्रशासनिक असंवेदनशीलता, स्थानीय जागरूकता की कमी और शोध संसाधनों का अभाव रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस शोध का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह शोध सिरोही ज़िले के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की पहचान, उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण, और विशेष रूप से चन्द्रावती की समृद्ध विरासत को उजागर करने का प्रयास करता है। इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: • सिरोही ज़िले के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त विश्लेषण: जिनमें अबू क्षेत्र, रोहिड़ा, पिंडवाड़ा, वेगड़ और अन्य स्थल शामिल हैं, जहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ, स्थापत्य अवशेष, मुद्राएँ तथा धार्मिक संरचनाएँ पाई गई हैं। • चन्द्रावती के ऐतिहासिक महत्व और पुरातात्विक संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन: नगर के उदय, विकास और पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख राजवंशों की भूमिका, तथा धार्मिक और सामाजिक जीवन के प्रमाणों का विश्लेषण। • चन्द्रावती की स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं नगर योजना का मूल्यांकन: मंदिरों की वास्तुशैली, मूर्तियों में अलंकरण की परंपरा, तोरण, स्तंभ और अधिष्ठानों की कलात्मकता, तथा नगर नियोजन की योजनाबद्धता को समझना। • क्षेत्र में पुरातत्व पर्यटन की संभावनाओं और संरक्षण की चुनौतियों की पहचान: पर्यटन विकास की संभावनाएँ, स्थानीय लोगों की भागीदारी, प्रशासनिक सहयोग, और संरक्षण नीति की आवश्यकता पर विमर्श। यह शोध न केवल अतीत को समझने का एक माध्यम है, बल्कि वर्तमान में सांस्कृतिक जागरूकता और भविष्य में धरोहरों के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। 3. शोध की विधि यह शोध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें तथ्य संकलन, क्षेत्रीय अध्ययन और साक्षात्कार जैसे विविध तरीकों का उपयोग किया गया है। शोध प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों का संतुलित उपयोग किया गया है, जिससे न केवल स्थल की ऐतिहासिकता को पुष्ट किया जा सके, बल्कि वर्तमान भौतिक स्थिति और संरक्षण की समस्याओं को भी समझा जा सके। प्राथमिक स्त्रोतों में सम्मिलित हैं: • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट्स: जिनमें चन्द्रावती क्षेत्र के उत्खनन, मूर्तिशिल्प, स्थापत्य और स्थल की ऐतिहासिकता से संबंधित प्रतिवेदन शामिल हैं। • क्षेत्रीय भ्रमण और स्थल अवलोकन: चन्द्रावती स्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्थल की संरचनाओं की फोटोग्राफी, बिखरे अवशेषों की स्थिति का मूल्यांकन, और स्थल-मानचित्रण। • स्थानीय अभिलेखागार एवं अभिलेख: शिलालेखों, ताम्रपत्रों, राजवंशीय अभिलेखों और स्थानीय जनश्रुतियों का संग्रह एवं अध्ययन। • स्थानीय नागरिकों, ग्रामीणों एवं पुरातत्व अधिकारियों के साक्षात्कार: क्षेत्र में जनमानस की जानकारी, ऐतिहासिक स्मृतियाँ, कथाएँ और परंपरागत विश्वासों का अभिलेखन। द्वितीयक स्त्रोतों में सम्मिलित हैं: • प्रकाशित पुस्तकें और शोध ग्रंथ: जिनमें चन्द्रावती, सिरोही और राजस्थान के पुरातत्व से संबंधित सामग्री समाहित है। इनमें पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा रचित कार्यों को विश्लेषण में शामिल किया गया। • शोध पत्र, जर्नल और कॉन्फ्रेंस पेपर्स: राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रासंगिक लेखों का संदर्भ। • विश्वविद्यालयों की थीसिस एवं शोध रिपोर्ट्स: जिनमें क्षेत्र विशेष पर केंद्रित स्नातकोत्तर एवं शोध प्रबंधों का अध्ययन किया गया। • ऑनलाइन डेटाबेस, पुरातत्व मानचित्र एवं संग्रहालय स्रोत: जहां से उपलब्ध चित्र, संरचनाओं की डिजिटाइज़ प्रतिलिपियाँ और वस्त्रावली प्राप्त की गई। इन सभी विधियों के माध्यम से एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया गया है, जिससे चन्द्रावती और सिरोही ज़िले के अन्य पुरातात्विक स्थलों को एक समग्र शोधात्मक दृष्टि से समझा जा सके। यह पद्धति शोध की निष्पक्षता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है। 4. सिरोही ज़िले के प्रमुख पुरातात्विक स्थल सिरोही ज़िला राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक अंचल है, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ समृद्ध पुरातात्विक धरोहर का केंद्र भी माना जाता है। इस ज़िले की भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक मार्गों से निकटता, और धार्मिक सहिष्णुता ने इसे प्राचीन समय में एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। यहां अनेक स्थलों पर प्राचीन काल की संस्कृति, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और सामाजिक जीवन के प्रमाण आज भी बिखरे पड़े हैं, जो न केवल स्थानीय इतिहास को समृद्ध करते हैं, बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी गहराई प्रदान करते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है: • अबू पर्वत क्षेत्र: अबू पर्वत सिरोही ज़िले का सबसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ स्थित जैन मंदिर, विशेषकर दिलवाड़ा मंदिर समूह, स्थापत्य और मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण हैं। इन मंदिरों की शिल्पकला, संगमरमर पर की गई महीन नक्काशी, स्तंभों और छतों पर अंकित धार्मिक दृश्य, मध्यकालीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यद्यपि ये मंदिर 11वीं–13वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे, परंतु इस क्षेत्र में इससे भी प्राचीन गुफाएँ, जल संरचनाएँ और पाषाण शिलालेख मिलते हैं जो इसकी पुरातात्विक महत्ता को प्रमाणित करते हैं। • झावरी, पिंडवाड़ा, रोहिड़ा: ये स्थल सिरोही ज़िले के अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक क्षेत्र हैं। यहाँ पर बौद्धकालीन टीलों, छोटे स्तूपों, मूर्तियों और शिलालेखों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह माना जाता है कि यह क्षेत्र मौर्य और शुंग काल में बौद्ध धर्म का एक उपकेंद्र था। साथ ही, बाद के काल में यहाँ पर शैव और वैष्णव धर्म की भी उपस्थिति देखने को मिलती है। • वेगड़: यह क्षेत्र मौर्य काल से संबद्ध टीलों, मुद्रा-अवशेषों और बिखरे हुए स्थापत्य खंडों के लिए जाना जाता है। यहाँ से मिले सिक्कों और मिट्टी के पात्रों के टुकड़े यह संकेत करते हैं कि यह स्थल एक प्राचीन बस्ती का हिस्सा रहा होगा। मौर्य और उत्तर-मौर्य कालीन संस्कृति के प्रमाण इस क्षेत्र को पुरातात्विक रूप से अत्यंत मूल्यवान बनाते हैं। • अजीतगढ़ दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र: अजीतगढ़ किला 15वीं शताब्दी में निर्मित एक सैन्य संरचना है, जो सिरोही के राजाओं के रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त खंडहरों, प्राचीरों, तोपों और कक्ष संरचनाओं से तत्कालीन किलेनिर्माण प्रणाली, निर्माण सामग्री, और सुरक्षा तंत्र का ज्ञान होता है। इन सभी स्थलों में विविध धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि इन पुरातात्विक स्थलों में चन्द्रावती की तुलना की जाए तो यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान के रूप में उभर कर सामने आता है। इसका कारण यह है कि चन्द्रावती न केवल स्थापत्य दृष्टि से समृद्ध रहा है, बल्कि नगर नियोजन, जल प्रबंधन, मूर्तिकला और शिल्प परंपरा का ऐसा अनूठा संगम यहाँ मिलता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। 5. चन्द्रावतीः ऐतिहासिक और पुरातात्विक विवेचन चन्द्रावती का उल्लेख प्राचीन साहित्य, राजवंशीय अभिलेखों और मध्यकालीन यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक यह नगर परमारों और बाद में सोलंकी वंश के अधीन था। परमार वंश ने इस नगर को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जहाँ मंदिरों, तोरणों, मूर्तियों और जल संरचनाओं का निर्माण हुआ। यह नगर धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक था, जहाँ शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध परंपराएँ एक साथ फलती-फूलती थीं। चन्द्रावती का पतन दिल्ली सल्तनत के पश्चिमी आक्रमणों, विशेषकर मुहम्मद ग़ोरी के हमलों के दौरान हुआ, जिसके कारण नगर के अधिकांश हिस्से नष्ट हो गए और शेष खंडहरों में परिवर्तित हो गए। 5.2 स्थल स्थिति और भौगोलिक महत्व चन्द्रावती सिरोही ज़िले के पिंडवाड़ा क्षेत्र के निकट बाणास नदी के तट पर स्थित है। यह नदी न केवल नगर की जलापूर्ति और कृषि का प्रमुख स्रोत थी, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी। चन्द्रावती का स्थान पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर था, जिससे यह नगर व्यापार, धर्म और संस्कृति का संगम बन सका। इसका निकटवर्ती संबंध गुजरात, मालवा और दक्षिण राजस्थान के अन्य व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों से रहा। 5.3 स्थापत्य एवं मूर्तिकला चन्द्रावती की स्थापत्य परंपरा मुख्यतः परमार शैली पर आधारित रही है, जिसमें मंदिरों में शिखर, मंडप, गर्भगृह और अलंकृत प्रवेशद्वारों का निर्माण किया गया। इस शैली में गजमुख, कीर्तिमुख, पल्लवित स्तंभ, नर्तकी आकृतियाँ और अलंकरण की बारीकियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ प्राप्त मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, जीवंत और तकनीकी दृष्टि से परिपक्व हैं। प्रमुख देवताओं में विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सूर्य, गणेश आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी विशिष्ट आभूषणों, लक्षणों और मुद्रा शुद्धता के साथ निर्मित हैं। 5.4 प्रमुख अवशेष और संरचनाएँ • तोरण द्वार: चन्द्रावती के प्रमुख प्रवेश द्वार के अवशेष आज भी स्थल पर बिखरे पड़े हैं। इन तोरणों में पशु आकृतियों, पुष्पावलियों और मिथुन मूर्तियों की सूक्ष्म नक्काशी है, जो परमारकालीन वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। • स्तंभ और अधिष्ठान: यहाँ के मंदिरों के पत्थर के स्तंभों में गंधर्व, अप्सरा, नर्तकी, और विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियों का अंकन मिलता है। अधिष्ठान भाग में पशु-मानव आकृतियों के अलावा धार्मिक कथाओं का भी चित्रण है। • जल प्रबंध: सरोवर, बावड़ियाँ, नालियाँ और कुंड इस बात के प्रमाण हैं कि चन्द्रावती में जल संचयन और वितरण की उन्नत प्रणाली थी। यह प्रणाली नगर की जीवनरेखा के रूप में कार्य करती थी और जल संकट से बचाव करती थी। 5.5 उत्खनन कार्य और नवीन खोजें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने चन्द्रावती में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक उत्खनन कार्य किया था, जिसमें मंदिरों, मूर्तियों, जल संरचनाओं और तोरणों के अवशेष सामने आए। वर्ष 2020 में एक निजी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में एक पुनरावलोकन परियोजना चलाई गई, जिसमें स्थल का डिजिटल स्कैनिंग, ड्रोन आधारित स्थल मानचित्रण, और त्रि-आयामी मॉडलिंग की गई। इन प्रयासों से स्थल की संरचनात्मक संरचना को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध हुआ। अजमेर संग्रहालय, सिरोही संग्रहालय और कुछ निजी संग्रहों में आज भी चन्द्रावती से प्राप्त मूर्तियाँ और शिलालेख संरक्षित हैं, जो न केवल इस नगर के कलात्मक वैभव को दर्शाते हैं, बल्कि इसके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों को भी उद्घाटित करते हैं। 6. चन्द्रावती में संरक्षण की स्थिति और चुनौतियाँ चन्द्रावती, सिरोही ज़िले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य की समृद्ध धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वर्तमान में इसकी भौतिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। यद्यपि इसके ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य को विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है, फिर भी यह स्थल संरक्षित स्थलों की प्राथमिक सूची में अपेक्षित स्थान नहीं पा सका है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ की बहुमूल्य मूर्तियाँ, स्थापत्य खंड और धार्मिक संरचनाएँ खुले में पड़ी हैं, उपेक्षित और क्षरण की अवस्था में। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अपर्याप्त जानकारी और जागरूकता के कारण, मंदिरों और मूर्तियों के पत्थरों का उपयोग अपने निर्माण कार्यों में कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर देखा गया है कि प्राचीन स्तंभों को घर की चौखट या ओटले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यटकों द्वारा स्थल पर की जाने वाली मनमानी गतिविधियाँ — जैसे स्मारकों पर नाम लिखना, तोरणों को नुकसान पहुँचाना, या मूर्तियों को छेड़ना — संरक्षण की राह में प्रमुख अवरोध हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय है प्रशासनिक उदासीनता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भले ही कुछ सीमित उत्खनन कार्य किए हों, परंतु स्थल की नियमित निगरानी, सुरक्षा और रखरखाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय कारकों जैसे वर्षा, मिट्टी का कटाव, वनस्पति विस्तार, और जीव-जंतुओं के कारण संरचनाएँ धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। प्रमुख चुनौतियाँ: • संरचनात्मक संरक्षण की अनुपस्थिति: वर्तमान में चन्द्रावती की संरचनाओं पर कोई स्थायी संरक्षण कार्य नहीं किया गया है। खंडहरों की मरम्मत, पुनर्स्थापना और संरक्षण की कोई स्पष्ट योजना नहीं है, जिससे स्थल की वर्तमान स्थिति और बिगड़ती जा रही है। • स्थानीय जागरूकता की कमी: क्षेत्रीय जनसमुदाय को चन्द्रावती के ऐतिहासिक महत्व की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस कारण न तो वे इसके संरक्षण के प्रति सजग हैं और न ही इसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। • स्पष्ट संरक्षण नीति का अभाव: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चन्द्रावती को एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने की कोई ठोस नीति नहीं है। इसके चलते यह स्थल विधिक रूप से भी संरक्षित नहीं है और किसी भी निर्माण, अतिक्रमण या क्षति के खिलाफ कोई प्रभावी रोक नहीं है। • शहरीकरण और सड़क निर्माण से हो रही क्षति: निकटवर्ती क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण, निर्माण गतिविधियाँ, और खनन कार्यों ने भी चन्द्रावती की संरचनाओं को नुकसान पहुँचाया है। कुछ अवशेषों के समीप हुई खुदाई से मूर्तियाँ टूट गईं और स्थल की स्थलाकृति में परिवर्तन आ गया। • अनौपचारिक खुदाई और चोरी: कुछ असंगठित तत्वों द्वारा चुपचाप मूर्तियों और कलाकृतियों की खुदाई कर उन्हें बाज़ार में बेचना भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इससे बहुमूल्य विरासत के चोरी हो जाने और पहचान से बाहर हो जाने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार चन्द्रावती का संरक्षण केवल एक पुरातात्विक दायित्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि समय रहते संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो यह बहुमूल्य धरोहर भविष्य में केवल पुस्तकों और संग्रहालयों तक सीमित रह जाएगी। 7. पर्यटन की संभावनाएँ चन्द्रावती में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, विशेषकर धरोहर पर्यटन (heritage tourism) और शैक्षणिक पर्यटन (educational tourism) के संदर्भ में। इसके पास स्थित माउंट आबू जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल की उपस्थिति इसे एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करती है। यदि इसे सही रूप में विकसित किया जाए, तो यह स्थल न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का साधन भी बन सकता है। वर्तमान में, पर्यटक माउंट आबू, आबू रोड और दिलवाड़ा मंदिरों तक ही सीमित रहते हैं। यदि चन्द्रावती को एक heritage trail के रूप में विकसित किया जाए, तो यह सिरोही ज़िले को एक नया पहचान-पथ दे सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार, पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय निकाय मिलकर समन्वित प्रयास करें। संभावित प्रयास: • डिजिटल सूचना केंद्र की स्थापना: एक इंटरएक्टिव डिजिटल संग्रहालय या सूचना केंद्र की स्थापना की जा सकती है जहाँ चन्द्रावती की मूर्तियों, स्थापत्य योजना, 3D स्कैनिंग और वर्चुअल टूर उपलब्ध हो। यह पर्यटकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। • साइन बोर्ड, गाइड सेवाएँ और प्रकाश व्यवस्था: स्थल पर समुचित सूचना पट्ट, मार्गदर्शन चिह्न, और शाम के समय सुंदर प्रकाश व्यवस्था इसे और प्रभावशाली बना सकती है। प्रशिक्षित गाइडों की सेवाएँ पर्यटकों को ज्ञानवर्धक अनुभव दे सकती हैं। • शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों की योजना: विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यालयों से सहयोग लेकर ऐतिहासिक भ्रमण (study tours), कार्यशालाएँ (workshops) और पुरातत्व विषयक प्रोजेक्ट्स कराए जा सकते हैं। इससे शैक्षणिक समुदाय को भी लाभ होगा और स्थानीय जागरूकता भी बढ़ेगी। • स्थानीय युवाओं को ‘heritage guide’ के रूप में प्रशिक्षण: स्थानीय युवाओं को पुरातत्व, इतिहास, मार्गदर्शन एवं संवाद-कला में प्रशिक्षित करके उन्हें "हेरिटेज गाइड" के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और पर्यटन का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुँचेगा। • स्थानीय हस्तशिल्प और स्मृति वस्त्रियों का विकास: चन्द्रावती से प्रेरित कलाकृतियाँ, मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ, और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित हस्तनिर्मित वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें पर्यटक स्मृति स्वरूप खरीद सकें। यदि इन प्रयासों को सुदृढ़ योजनाओं और कार्यान्वयन के साथ जोड़ा जाए, तो चन्द्रावती आने वाले वर्षों में सिरोही ज़िले का सांस्कृतिक प्रतीक बन सकती है, एक ऐसा स्थल जो अतीत की भव्यता और वर्तमान की चेतना के मध्य सेतु का कार्य करे। 8. निष्कर्ष चन्द्रावती, सिरोही ज़िले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की एक ऐसी अमूल्य कड़ी है, जो आज उपेक्षा, असंवेदनशीलता और संरचनात्मक क्षरण के कारण बिखरती हुई प्रतीत होती है। यह स्थल केवल खंडहरों का समूह नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय नगर नियोजन, स्थापत्य कला, मूर्तिशिल्प, धार्मिक सहिष्णुता और व्यापारिक समृद्धि का जीवंत प्रतीक रहा है। यहाँ की परमार और सोलंकी कालीन स्थापत्य शैली, विस्तृत तोरण द्वार, अलंकृत मूर्तियाँ, और सुव्यवस्थित जल प्रबंधन प्रणाली, इस नगर को एक परिपक्व एवं विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। इतिहास को यदि वर्तमान से जोड़ा न जाए, तो वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। चन्द्रावती आज इसी स्थिति में है — जहां स्मृतियाँ तो हैं, पर उनकी देखरेख, संरक्षण और प्रसार के समुचित प्रयास नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सीमित उत्खनन और स्थानीय संग्रहालयों में कुछ मूर्तियों के संरक्षण से आगे कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता, जन-जागरूकता की कमी और तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, इस स्थल को लगातार हानि पहुँचा रहे हैं। शोध में यह स्पष्ट हुआ है कि सिरोही ज़िले में अनेक ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो अभी तक अनुसंधान और संरक्षण के दायरे में पूरी तरह नहीं आ सके हैं। परंतु इन सभी में चन्द्रावती अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत के कारण एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह स्थल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, स्थापत्य विशेषज्ञों, पर्यटकों और स्थानीय समुदाय — सभी के लिए मूल्यवान है। भविष्य की दृष्टि से, यदि चन्द्रावती को एक संरक्षित पुरातात्विक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए, तो यह न केवल शोध एवं अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय आर्थिक विकास के एक सशक्त केंद्र के रूप में भी उभरेगा। इसके लिए डिजिटल संरक्षण, व्यापक प्रचार, स्थानीय सहभागिता और स्पष्ट संरक्षण नीति की नितांत आवश्यकता है। चन्द्रावती का संरक्षण केवल पत्थरों की रक्षा नहीं, बल्कि हमारी उस सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना है, जो भारत की आत्मा को परिभाषित करती है। यह हमारी साझा ज़िम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को केवल अतीत का अवशेष बनकर न रहने दें, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और अध्ययन का जीवंत केंद्र बनाएँ। 9. संदर्भ सूची (References) 1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI). चन्द्रावती उत्खनन रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1994–2002. 2. शर्मा, आर.एस. (2003). प्राचीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास. दिल्ली: मकमिलन इंडिया लिमिटेड. 3. सिंह, उपेंद्र. (2012). Ancient India: Culture and Thought. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. पृष्ठ: 198–214. 4. मेहता, जे.सी. (1990). Rajasthan Through the Ages: From Prehistoric Times to 1200 A.D. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर. पृष्ठ: 172–195. 5. Jain, K.C. (1998). Ancient Cities and Towns of Rajasthan: A Study of Culture and Civilization. न्यू दिल्ली: पौराणिक प्रकाशन. पृष्ठ: 45–67. 6. गोस्वामी, श्याम सुंदर. (2007). राजस्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण. जयपुर: जयपुर विश्वविद्यालय प्रकाशन. पृष्ठ: 85–108. 7. Indian Archaeology – A Review (IAR). Annual Reports (1980–2010). Archaeological Survey of India. 8. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार. चन्द्रावती क्षेत्रीय रिपोर्ट (2005). अजमेर मंडल कार्यालय। 9. Chandravati Heritage Mapping Project Report. (2021). Department of History and Archaeology, JRN Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur. 10. Gupta, P.L. (2001). Coins and Currency Systems in Ancient India. वाराणसी: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस. पृष्ठ: 92–97. 11. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR). भारत के प्राचीन नगर: एक पुरातात्विक अध्ययन. नई दिल्ली: परिषद प्रकाशन. पृष्ठ: 121–139. 12. Desai, Devangana. (1996). Art and Icon: Essays on Early Indian Art. मुंबई: मार्ग पब्लिकेशन. पृष्ठ: 73–89. 13. Ray, Himanshu Prabha. (2008). The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. पृष्ठ: 151–159. 14. Local Interviews (2022). ग्रामीण बुजुर्गों, मंदिर संरक्षकों एवं स्थानीय पुरातत्वकर्मियों से व्यक्तिगत बातचीत एवं स्थल भ्रमण से प्राप्त जानकारी। 15. Google Earth & Digital Mapping Data (2020–2023). Chandravati Site Survey and Geo-Tagging. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
| Cite This | सिरोही के पुरातात्विक स्थलः चन्द्रावती के विशेष संदर्भ में - SOHAN LAL - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

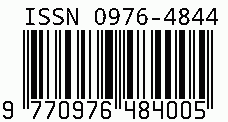
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

