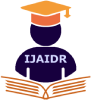
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
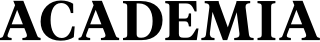













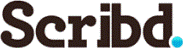




राजस्थान की जलवायु प्रवृत्तियाँ और उनके कृषि एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव: एक दीर्घकालिक अध्ययन
| Author(s) | Ayush Soni |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, विविध स्थलाकृतियों और जलवायु रूपों के कारण एक विशिष्ट पर्यावरणीय भूगोल प्रस्तुत करता है। यहाँ पश्चिम में विस्तृत थार मरुस्थल की तपती रेत है, तो दक्षिण और पूर्व में अरावली पर्वतमालाएँ हरियाली और नमी का संकेत देती हैं। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः अर्ध-शुष्क और शुष्क श्रेणियों में आती है, जहाँ तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव और वर्षा की अनिश्चितता प्रमुख लक्षण हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान 48°C तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान कभी-कभी शून्य के आसपास भी दर्ज किया जाता है। औसतन, राजस्थान को 100 से 600 मिमी तक ही वर्षा प्राप्त होती है, वह भी अत्यंत असमान रूप से—कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा रहता है, तो कहीं-कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। मानसूनी हवाओं का प्रभाव भी समय के साथ अस्थिर होता गया है। इसके कारण न केवल कृषि के फसल चक्र पर, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और जल संसाधनों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ दशकों के जलवायु डेटा का अध्ययन यह संकेत देता है कि राजस्थान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और सूखे की आवृत्ति बढ़ी है। यह दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन एक चेतावनी है, विशेषकर एक ऐसे राज्य के लिए जो पहले से ही सीमित जल संसाधनों, कम वर्षा और भूमि क्षरण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस शोध-पत्र के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि राजस्थान की जलवायु में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ उभरकर सामने आई हैं, और इन प्रवृत्तियों का राज्य की कृषि प्रणाली, पारिस्थितिकीय तंत्र, मानव जीवन एवं पर्यावरणीय स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि किन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक गहरा है, और किस प्रकार के अनुकूलन उपाय आवश्यक हैं। 2. शोध की आवश्यकता (Need of the Study) जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की ठोस सच्चाई है, और राजस्थान जैसे संवेदनशील राज्य में इसके प्रभाव पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। यहाँ की लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और जब वर्षा का स्वरूप बदलता है, तापमान बढ़ता है, या मानसून अस्थिर होता है, तो पूरे ग्रामीण तंत्र पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में, जहाँ पहले ही पानी की भारी कमी है, जलवायु परिवर्तन ने सिंचाई प्रणालियों को अस्थिर कर दिया है। मिट्टी की नमी में कमी, भूमिगत जल स्तर का गिरना, और जलाशयों का सूख जाना – ये सभी संकेत हैं कि जलवायु संकट वास्तविक है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में भी अनियमित वर्षा और बाढ़ की घटनाएँ कृषि को क्षतिग्रस्त कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक फसलें अब पूर्व की तरह उत्पादन नहीं दे पा रही हैं। साथ ही, कई फसलों का कृषि क्षेत्र सिमटता जा रहा है, और किसान अधिक जोखिम वाले विकल्पों की ओर जा रहे हैं। पशुपालन, जो राज्य का एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, भी जल और चारे की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्तियों का दीर्घकालिक अध्ययन किया जाए – विशेष रूप से तापमान, वर्षा, चरम मौसमी घटनाएँ (जैसे लू, ओलावृष्टि, सूखा) और इनके स्थानिक प्रभाव को समझा जाए। यह अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि: • राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाओं में वैज्ञानिक जलवायु डेटा का अभाव है। • कृषि नीति और सिंचाई योजनाएँ अभी भी पारंपरिक अनुमानों पर आधारित हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। • पारिस्थितिकीय क्षरण की दर बढ़ रही है, और जैव विविधता पर जलवायु प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है। • जलवायु-लचीली (Climate-Resilient) रणनीतियों की नींव तभी रखी जा सकती है जब हमें स्पष्ट और स्थानिक विश्लेषण उपलब्ध हो। इस शोध का निष्कर्ष केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति निर्धारकों, कृषि योजनाकारों, पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों के लिए भी दिशा निर्देश प्रस्तुत कर सकता है। यदि हम समय रहते इन प्रवृत्तियों की पहचान कर समाधान प्रस्तुत करें, तो राजस्थान जैसे संवेदनशील राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 3. उद्देश्य (Objectives) राजस्थान की जलवायु प्रवृत्तियों और उनके कृषि एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों को समझना एक बहुआयामी दृष्टिकोण की माँग करता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज, आजीविका और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के भीतर बदलती जलवायु प्रवृत्तियों का दीर्घकालिक विश्लेषण करना और इनसे उत्पन्न कृषि एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों की व्यापक समीक्षा करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: 1. राजस्थान में पिछले 50 वर्षों की जलवायु प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना, जिसमें वर्षा की मात्रा और वितरण, औसत तथा चरम तापमानों में बदलाव, और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति (जैसे लू, सूखा, बाढ़) की प्रवृत्तियाँ शामिल हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के स्वरूप की दीर्घकालिक समझ विकसित की जा सकेगी। 2. जलवायु परिवर्तन का कृषि तंत्र पर प्रभाव स्पष्ट करना, जैसे फसल चक्र में बदलाव, फसल उत्पादन की मात्रा में उतार-चढ़ाव, सिंचाई संसाधनों पर बढ़ता दबाव, और कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में गिरावट। 3. राज्य के पारिस्थितिकीय तंत्र पर जलवायु अस्थिरता के प्रभावों का आकलन करना, जिसमें वनस्पति संरचना, स्थानीय एवं प्रवासी जैव विविधता, जल स्रोतों की स्थायित्व क्षमता, वनों का संकुचन, और चारागाह क्षेत्रों की हानि शामिल है। 4. क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु-लचीले (climate-resilient) उपायों की पहचान करना, जिनमें कृषि में जैविक पद्धतियाँ, सूखा-सहिष्णु फसलें, जल संरक्षण तकनीकें और सामुदायिक अनुकूलन मॉडल शामिल हैं। 5. राज्य-स्तरीय दीर्घकालिक कृषि एवं पर्यावरणीय नीति निर्माण हेतु व्यवहारिक अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना, जिससे कृषि उत्पादकता, जल संसाधन प्रबंधन और पारिस्थितिकीय संतुलन में संतुलित विकास संभव हो सके। 4. अध्ययन क्षेत्र का परिचय (Study Area Overview) राजस्थान राज्य, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है, लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य की जलवायु, स्थलाकृति और पारिस्थितिकी में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जो इसे जलवायु अध्ययन के लिए एक आदर्श केस स्टडी बनाती है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को चार प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक की जलवायु प्रवृत्तियाँ और कृषि-पर्यावरणीय स्थितियाँ भिन्न हैं: 1. पश्चिमी शुष्क क्षेत्र (Western Arid Zone) जिलों में शामिल: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर का पश्चिमी भाग • यहाँ की वार्षिक वर्षा 100–200 मिमी के बीच होती है, वह भी अत्यंत असमान और अनिश्चित रूप से। • थार मरुस्थल इस क्षेत्र का प्रमुख भौगोलिक अंग है। • दिन और रात के तापमान में भारी अंतर रहता है। • मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक यहीं पर दृष्टिगोचर होता है। 2. अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semi-Arid Zone) जिलों में शामिल: जोधपुर, नागौर, अजमेर, चुरू • यहाँ की वर्षा लगभग 200–400 मिमी होती है। • यह क्षेत्र स्थलाकृतिक दृष्टि से पठारी और मैदानी है, जहाँ मानसून पर निर्भर कृषि होती है। • सिंचाई की निर्भरता भूमिगत जल पर अधिक है, जो लगातार घट रहा है। • तापमान की अस्थिरता के कारण रबी फसलों को अधिक क्षति होती है। 3. पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र (Eastern Fertile Zone) जिलों में शामिल: कोटा, झालावाड़, बारां, भरतपुर, धौलपुर • यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत अधिक (~600–900 मिमी) होती है। • चंबल बेसिन के कारण यहाँ सिंचाई सुविधाएँ विकसित हैं। • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इस क्षेत्र में अधिक वर्षा और कभी-कभी बाढ़ के रूप में देखे जाते हैं। • गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती हैं। 4. दक्षिणी आद्र क्षेत्र (Southern Humid Zone) जिलों में शामिल: उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ • यहाँ मानसून की सक्रियता अधिक है और वर्षा लगभग 900–1000 मिमी तक हो सकती है। • अरावली पर्वतमाला इस क्षेत्र को हरित और जल-सम्पन्न बनाती है। • जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा के स्वरूप में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कटाव, भूस्खलन और फसल क्षति की घटनाएँ बढ़ी हैं। यह विविधता न केवल जलवायु परिवर्तन की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि एक समान रणनीति राज्य के सभी हिस्सों में लागू नहीं की जा सकती। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र के लिए पृथक और उपयुक्त अनुकूलन उपाय आवश्यक हैं। 5. जलवायु प्रवृत्तियों का दीर्घकालिक विश्लेषण (Long-Term Climatic Trends) राजस्थान जैसे जल-संवेदनशील राज्य में जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD), कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), और राष्ट्रीय जल आयोग जैसे संस्थानों द्वारा एकत्रित आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में पिछले पाँच दशकों में जलवायु के स्वरूप में महत्वपूर्ण और चिंताजनक बदलाव आए हैं। नीचे वर्षा, तापमान और चरम मौसमी घटनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दी गई हैं: 5.1 वर्षा प्रवृत्तियाँ (Rainfall Trends) राजस्थान की वर्षा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून पर आधारित होती है, जो जून के अंत से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। किन्तु बीते 50 वर्षों (1971–2020) के आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हुई हैं: • औसत वर्षा में गिरावट: राज्य में औसत वार्षिक वर्षा में लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में यह गिरावट और अधिक गंभीर है। वहीं, कुछ पूर्वी जिलों में कुल वर्षा की मात्रा स्थिर रही है, किंतु वितरण अनियमित होता गया है। • वर्षा वितरण में असमानता: अब वर्षा की घटनाएँ कम बार होती हैं लेकिन अत्यधिक तीव्रता के साथ होती हैं। उदाहरण के लिए, कहीं-कहीं 24 से 48 घंटे में पूरी मौसमी वर्षा हो जाती है, जबकि शेष समय सूखा रहता है। • मानसून की अनिश्चितता: मानसून का आगमन औसतन 7–10 दिनों की देरी से होता है। कई वर्षों में मानसून की सक्रियता बहुत कम समय तक रह जाती है, जिससे खेती का पूरा चक्र प्रभावित होता है। • Post-Monsoon और Pre-Monsoon वर्षा की घटनाएँ अस्थिर होती गई हैं, जिससे रबी फसलों की सिंचाई पर प्रभाव पड़ा है। प्रभाव: • बुआई की समय-सारणी में परिवर्तन। • वर्षा पर आधारित सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादकता में गिरावट। • वर्षा जल संचयन की योजनाओं की विफलता। 5.2 तापमान में वृद्धि (Temperature Rise) राज्य के जलवायु डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में तापमान बढ़ोतरी अब एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति बन चुकी है। • औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि: 1971 से 2020 के बीच औसत वार्षिक तापमान में लगभग 1.2°C की वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषतः गर्मी के महीनों (मार्च-जून) में यह वृद्धि अधिक तीव्र है। • गर्मी की लहरों (Heatwaves) में बढ़ोतरी: जयपुर, चूरू, बीकानेर, और जोधपुर जैसे शहरों में हर वर्ष औसतन 5–7 दिन अधिक लू चलने लगी है। उदाहरण: चुरू ने 2019 में 50°C का रिकॉर्ड दर्ज किया। • न्यूनतम (रात्रि) तापमान में वृद्धि: रात्रि तापमान में वृद्धि से evapotranspiration की दर बढ़ी है, जिससे मिट्टी की नमी में तेज़ी से कमी आती है। इसका असर विशेषतः सब्ज़ी व बागवानी फसलों पर पड़ता है, जो रात में तापमान स्थिरता पर निर्भर करती हैं। प्रभाव: • मिट्टी का अधिक शुष्क हो जाना और सिंचाई की मांग में वृद्धि। • पशुधन पर गर्मी का प्रभाव — दूध उत्पादन में गिरावट। • गर्मियों की फसलों पर सीधा प्रभाव: ज्वार, बाजरा, मूंग की उत्पादकता घटी। 5.3 चरम मौसमी घटनाएँ (Extreme Weather Events) राजस्थान में चरम मौसम घटनाओं (Extreme Events) की आवृत्ति में भी स्पष्ट वृद्धि देखी गई है, जिससे कृषि और पारिस्थितिकी दोनों पर खतरा बढ़ा है। • सूखा (Drought): प्रमुख सूखा-वर्ष – 1979, 1987, 2002, 2015, 2018 इन वर्षों में 20 से अधिक जिलों में वर्षा सामान्य से 40% कम दर्ज की गई थी। • अतिवृष्टि और बाढ़: पूर्वी राजस्थान (कोटा, बाराँ, भरतपुर, दौसा) में 2017 और 2023 में बाढ़ की घटनाएँ सामने आईं। कारण: कम समय में अत्यधिक वर्षा — जल निकासी प्रणाली की विफलता। परिणाम: रबी फसलें प्रभावित, ग्रामीण सड़कों और खेतों का कटाव। • ओलावृष्टि और पाला (Hailstorm and Frost): फरवरी–मार्च में ओलावृष्टि की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे रबी की फसलों को नुकसान हुआ है (जैसे सरसों, चना, गेहूं)। पाले की घटनाओं ने विशेषकर दक्षिण राजस्थान (उदयपुर, प्रतापगढ़) में सब्ज़ी उत्पादन को नुकसान पहुँचाया। राजस्थान की जलवायु प्रवृत्तियों में यह दीर्घकालिक परिवर्तन अब सतही नहीं, बल्कि प्रणालीगत हैं। तापमान में निरंतर वृद्धि, वर्षा में अनिश्चितता, और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति का बढ़ना संकेत करता है कि राज्य को अब जलवायु-अनुकूल कृषि एवं पर्यावरण रणनीतियों की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाने होंगे। 6. कृषि पर प्रभाव (Impact on Agriculture) राजस्थान में जलवायु प्रवृत्तियों में आए दीर्घकालिक बदलावों का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर देखा गया है, जो राज्य की 70% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का आधार है। पारंपरिक कृषि चक्र, फसल चयन, उत्पादन पद्धतियाँ और सिंचाई ढांचे जलवायु के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहे हैं। नीचे प्रमुख प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत है: 1. फसल उत्पादन में गिरावट जलवायु अस्थिरता विशेषकर रबी फसलों पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। • गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों में औसतन 15–25% तक उत्पादकता की कमी देखी गई है। • वर्षा की असमानता और न्यून तापमान की अनुपस्थिति से flowering और grain-filling चरण प्रभावित होते हैं। 2. फसल चक्र में अनिश्चितता • खरीफ सीजन में मानसून की देर से शुरुआत के कारण बुवाई 1–3 सप्ताह तक विलंबित होती है। • कई बार पर्याप्त वर्षा न होने से बीज अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे किसान पुनः बुआई नहीं कर पाते। 3. पारंपरिक फसलों में गिरावट • पहले उगाई जाने वाली बाजरा, मोठ, ग्वार जैसी फसलें अब कम हो गई हैं। • इनके स्थान पर अल्पावधि और market-dependent फसलें जैसे टमाटर, हरा धनिया, मूंगफली आ रही हैं, जो जलवायु के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। • इससे खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक आहार संरचना प्रभावित हुई है। 4. पशुधन पर प्रभाव • चारे की उपलब्धता में 30–40% तक कमी आई है, विशेषकर सूखे वर्षों में। • जल स्रोतों के सूखने से मवेशियों के लिए पानी का संकट गहराया है। • अत्यधिक तापमान और लू के कारण पशु-स्वास्थ्य में गिरावट, दुग्ध उत्पादन में कमी, और रोग-प्रसार की आशंका बढ़ी है। 5. सिंचाई संकट • भूमिगत जल स्तर में औसतन 2–5 मीटर प्रति दशक की गिरावट देखी गई है। • कुएँ और नलकूप सूखने लगे हैं। • नहर सिंचाई प्रणाली पर दबाव बढ़ा है, जिससे पानी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती। निष्कर्षतः, राजस्थान की कृषि प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यदि इन प्रवृत्तियों पर तुरंत ध्यान न दिया गया तो यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक संकट की ओर धकेल सकता है। 7. पारिस्थितिकीय प्रभाव (Ecological Impacts) जलवायु परिवर्तन केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता तक फैला हुआ है। राजस्थान जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र में छोटे-छोटे बदलाव भी प्राकृतिक पर्यावरण पर गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। 1. वनस्पति परिवर्तन • उच्च तापमान और वर्षा की कमी से xerophytic यानी शुष्क जलवायु सहिष्णु पौधों का वर्चस्व बढ़ रहा है। • खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा जैसे वृक्षों की सूखने की दर में वृद्धि हो रही है। • घास प्रजातियों की विविधता में 20–30% की गिरावट दर्ज की गई है। 2. जल निकायों की सिकुड़न • झीलें और तालाब—जैसे पुष्कर झील, फतेहसागर, और ग्रामीण तालाब—मॉनसून में भर नहीं पा रहे हैं। • गांवों के पारंपरिक जल स्रोत (जोहड़, टांके) अब मौसमी बन गए हैं, जिससे ग्रामीण पारिस्थितिकी अस्थिर हो रही है। 3. जैव विविधता में कमी • प्रवासी पक्षियों (जैसे साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के आगमन में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। • शुष्क वन्यजीव जैसे नीलगाय, चिंकारा, लोमड़ी आदि का प्रवास क्षेत्र सिकुड़ रहा है। • जलस्रोतों की कमी से aquatic biodiversity जैसे मछलियों, कीटों की प्रजातियाँ कम हो रही हैं। 4. मरुस्थलीकरण की गति • पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण की दर 5,000–6,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष आँकी गई है। • जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में कृषि भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना बढ़ा है। • मृदा की उपजाऊता घट रही है और desert creep की समस्या उत्पन्न हो रही है। 5. मृदा क्षरण • अरावली पर्वत श्रंखला में अनियमित वर्षा के कारण जल अपरदन और कटाव की घटनाएँ बढ़ी हैं। • वनस्पति आवरण के क्षीण होने से top soil का नाश हो रहा है, जिससे खेतों की उर्वरता में गिरावट आई है। जलवायु परिवर्तन न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि राज्य की पारिस्थितिक स्थिरता और दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डालता है। 8. सुझाव (Suggestions) राजस्थान में जलवायु प्रवृत्तियों के प्रभाव को देखते हुए, अब यह आवश्यक हो गया है कि कृषि और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक रणनीतियाँ अपनाई जाएँ। नीचे कुछ प्रमुख सुझाव दिए जा रहे हैं: 1. जलवायु-लचीली कृषि प्रणाली का विकास (Climate-Resilient Agriculture) • कारण: बदलती वर्षा और बढ़ते तापमान ने पारंपरिक फसल चक्र को अस्थिर बना दिया है। • उपाय: o सूखा-सहिष्णु एवं अल्पकालिक फसलों (जैसे बाजरा, मूँग, मोठ) को बढ़ावा देना। o फसल विविधीकरण (Crop Diversification) अपनाना, जिससे एक ही समय में कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकें। o बागवानी, औषधीय पौधों एवं कम जल आवश्यकताओं वाली फसलों को शामिल करना। • लाभ: किसान की आय में स्थिरता, जल पर निर्भरता में कमी, खाद्य सुरक्षा में सुधार। 2. जल प्रबंधन सुधार (Water Management Enhancement) • कारण: वर्षा की असमानता और भूजल स्तर में गिरावट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। • उपाय: o वर्षा जल संचयन को गांव और खेत स्तर पर अनिवार्य करना। o टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक को प्रोत्साहित करना। o जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) बढ़ाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण देना। • लाभ: सिंचाई जल की बचत, भूजल पुनर्भरण, फसल लागत में कमी। 3. पारिस्थितिक पुनर्वनीकरण (Ecological Restoration) • कारण: पारिस्थितिकीय असंतुलन और मरुस्थलीकरण की गति को रोकना अत्यंत आवश्यक है। • उपाय: o स्थानीय शुष्क क्षेत्रीय पौधों (जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल) का वृक्षारोपण। o चारागाहों का संरक्षण एवं साइलेज आधारित पशु आहार योजनाओं को बढ़ावा देना। o वनों के पुनःस्थापन हेतु सामुदायिक वन प्रबंधन समितियाँ बनाना। • लाभ: जैव विविधता का संरक्षण, मृदा अपरदन में कमी, पशुधन को चारा सुरक्षा। 4. जलवायु-सूचक तंत्र का विकास (Local Climate Indicators & Early Warning Systems) • कारण: किसानों को समय पर मौसम की जानकारी न मिल पाने से हानि होती है। • उपाय: o ग्राम स्तर पर मौसम पूर्वानुमान सूचना केंद्र की स्थापना। o मोबाइल आधारित जलवायु चेतावनी प्रणाली विकसित करना। o कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण। • लाभ: किसान निर्णय लेने में सक्षम होगा, जोखिम में कमी आएगी, फसल नुकसान घटेगा। 5. नीति और संस्थागत समर्थन (Policy and Governance Support) • कारण: राजस्थान में अब तक जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित नीति क्रियान्वयन की गति धीमी रही है। • उपाय: o ‘राजस्थान जलवायु अनुकूलन नीति’ की स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी। o जलवायु-अनुकूल बीमा योजनाओं और अनुदानों का प्रभावी कार्यान्वयन। o जिलावार कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro-Climatic Zoning) के अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन। • लाभ: योजनाओं की दक्षता में वृद्धि, नीति और ज़मीनी कार्यान्वयन में सामंजस्य, संसाधनों का लक्ष्य आधारित उपयोग। इन उपायों को यदि समन्वित रूप से लागू किया जाए — जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परंपरागत ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत किया जाए — तो राजस्थान की कृषि और पारिस्थितिकी दोनों को जलवायु जोखिमों से बचाया जा सकता है। 9. निष्कर्ष (Conclusion) राजस्थान की जलवायु प्रवृत्तियाँ – जैसे औसत तापमान में वृद्धि, वर्षा में अनियमितता, सूखा चक्र की आवृत्ति में वृद्धि, और चरम मौसमीय घटनाओं में तीव्रता – अब केवल मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। इस दीर्घकालिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्थान की कृषि व्यवस्था पर पड़ा है। पारंपरिक फसलों की उत्पादकता में गिरावट, फसल चक्र में अस्थिरता, भूजल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था की हानि – ये सब राज्य के लाखों किसानों की आजीविका को संकट में डाल रहे हैं। साथ ही, पारिस्थितिकीय स्तर पर वनस्पति आवरण का क्षरण, मरुस्थलीकरण की गति में वृद्धि, जल निकायों का सिकुड़ना, और जैव विविधता में कमी यह दर्शाते हैं कि राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की पारिस्थितिक संतुलनकारी भूमिका भी कमजोर पड़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन को केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक और नीतिगत चुनौती के रूप में देखा जाए। राज्य में जलवायु-लचीले कृषि मॉडल, स्थानीय जल प्रबंधन, पारिस्थितिक पुनरुत्थान, और जनसहभागिता पर आधारित नीतियाँ तत्काल लागू की जानी चाहिए। यदि राजस्थान को जलवायु संकट से प्रभावी रूप से उबारना है, तो आवश्यक होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति निर्माण और सामाजिक भागीदारी – इन तीनों स्तरों पर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाए। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आने वाली पीढ़ियाँ एक अधिक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध जलवायु प्रणाली की उत्तराधिकारी बनें। 10. संदर्भ सूची (References) 1. Government of Rajasthan. (2021). Rajasthan State Action Plan on Climate Change (SAPCC). Department of Environment and Climate Change, Government of Rajasthan. pp. 12–27, 56–68 2. IMD (Indian Meteorological Department). (2020). Climatological Normals of Rajasthan (1981–2010). Ministry of Earth Sciences, Government of India. pp. 45–63 3. Central Ground Water Board (CGWB). (2022). Ground Water Year Book – Rajasthan. Ministry of Jal Shakti, Government of India. pp. 14–32, 75–81 4. Singh, R. B. (2019). Climate Change and Agriculture in Arid Rajasthan. Indian Journal of Geography and Environment. Vol. 42. pp. 102–118 5. Sharma, D. & Meena, M. L. (2020). Impact of Climate Variability on Agriculture in Rajasthan. Journal of Climatology and Agricultural Planning. Vol. 35(2). pp. 60–77 |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
| Cite This | राजस्थान की जलवायु प्रवृत्तियाँ और उनके कृषि एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव: एक दीर्घकालिक अध्ययन - Ayush Soni - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

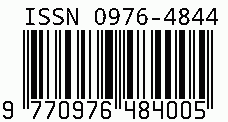
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

