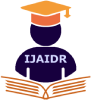
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
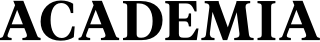













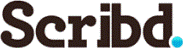




राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएँ, कारण और नियंत्रण उपाय: एक पर्यावरणीय भूगोलीय अध्ययन
| Author(s) | Shipra Vyas |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | राजस्थान, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस विशाल प्रदेश का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 2.1 लाख वर्ग किमी) क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु से प्रभावित है, जहाँ औसतन वर्षा 100 से 500 मिमी/वर्ष के बीच होती है। इन कठोर जलवायु परिस्थितियों में भी राज्य में वर्षों से मानव बसावट, कृषि और पशुपालन की परंपरा चली आ रही है। हालांकि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण नियंत्रण केंद्र (NRSC) द्वारा 2021 में प्रकाशित Desertification and Land Degradation Atlas of India के अनुसार, राजस्थान का 61.31% क्षेत्र मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण से प्रभावित है, जो देश में सर्वाधिक है। तालिका 1: राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित भूमि (2021 के अनुसार) क्रम जिला कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (किमी²) मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र (किमी²) प्रतिशत (%) 1 जैसलमेर 38,401 35,229 91.74 2 बाड़मेर 28,387 25,984 91.52 3 बीकानेर 30,247 26,145 86.44 4 नागौर 17,718 14,030 79.18 5 जोधपुर 22,850 17,136 74.97 राजस्थान (कुल) 3,42,239 2,10,000 (लगभग) 61.31 स्रोत: ISRO - Desertification Atlas, 2021; NRSC Hyderabad इस भयावह परिदृश्य के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारण सक्रिय हैं—जैसे कि असंतुलित भूमि उपयोग, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन, और बेतरतीब कृषि विस्तार। परिणामस्वरूप राजस्थान के कई भागों में भूमि की उत्पादकता घट रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, और स्थानीय आबादी का पलायन बढ़ रहा है। कृषि और जल पर प्रभाव: राजस्थान की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और इस परिघटना से उनकी आजिविका सीधी प्रभावित हो रही है। मरुस्थलीकरण से सिंचाई योग्य भूमि में कमी आती है और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता है, जिससे खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रभाव: रेत के टिब्बों का विस्तार, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, और पारंपरिक वनस्पतियों का लोप जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए, खेजड़ी जैसे स्थानीय वृक्ष जिनका पारिस्थितिक व सांस्कृतिक महत्व है, अब कम होते जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह शोध-पत्र मरुस्थलीकरण की प्रमुख प्रक्रियाओं, उनके प्रभावकारक कारणों, और उपयुक्त नियंत्रण उपायों का एक पर्यावरणीय भूगोल के परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य इस जटिल चुनौती के समाधान हेतु नीतिगत, वैज्ञानिक और सामुदायिक प्रयासों की दिशा में ठोस सिफारिशें देना है ताकि सतत विकास और पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके 2. शोध की आवश्यकता (Need of the Study) मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया राजस्थान के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रही है। भूमि की उत्पादकता में गिरावट, जलवायु में कठोरता, जैव विविधता का हास, और खाद्य असुरक्षा इस प्रक्रिया के प्रमुख दुष्परिणाम हैं। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो राज्य के कृषि और जल संसाधन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति, कारण और प्रभाव अलग-अलग हैं, जिन्हें क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के समन्वय से नियंत्रण उपायों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 3. उद्देश्य (Objectives) 1. राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रमुख प्रक्रियाओं की भौगोलिक पहचान करना। 2. मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक व मानवजनित कारणों का विश्लेषण करना। 3. मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण और विस्तार मापना। 4. वर्तमान में अपनाए जा रहे नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन करना। 5. पर्यावरणीय संतुलन हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना। 4. अध्ययन क्षेत्र का परिचय (Overview of Study Area) राजस्थान, भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित, एक विशाल और भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.41% है। इस विशाल भूभाग का लगभग 60% (करीब 2 लाख वर्ग किमी) क्षेत्रफल थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जो भारत का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। राज्य के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिले, जैसे: • जैसलमेर • बाड़मेर • बीकानेर • जोधपुर • नागौर • श्रीगंगानगर मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100–300 मिमी के बीच होती है, जो अत्यंत अल्प है। साथ ही, तापमान का अंतर भी बहुत अधिक होता है—गर्मी में 50°C तक और सर्दी में 4°C तक पहुँच सकता है। यह जलवायु विविधता मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करती है। भौगोलिक विशेषताएँ: • अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में फैली है, राज्य को पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय भाग और पूर्वी अर्ध-शुष्क एवं उपजाऊ भाग में विभाजित करती है। • पूर्वी राजस्थान—जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर—में औसत वर्षा 600–1000 मिमी तक होती है, जिससे यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक कृषि उपयुक्त है। • वहीं पश्चिमी राजस्थान में रेतीले टिब्बे, अल्प वनस्पति, और तेज हवाओं की अधिकता भूमि की अपरदन और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। तालिका 2: मरुस्थलीकरण से प्रभावित प्रमुख जिले (ISRO, 2021 के अनुसार) क्रम जिला कुल क्षेत्रफल (किमी²) मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र (%) 1 जैसलमेर 38,401 91.74% 2 बाड़मेर 28,387 91.52% 3 बीकानेर 30,247 86.44% 4 नागौर 17,718 79.18% 5 जोधपुर 22,850 74.97% 6 श्रीगंगानगर 11,154 67.23% स्रोत: ISRO & NRSC, 2021 - Desertification Atlas of India पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र: • इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के प्रभाव से कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली बढ़ी है, लेकिन अत्यधिक सिंचाई और जलभराव के कारण मृदा क्षारीयता और लवणता बढ़ी है। • ओरण, गऊचार भूमि और चारागाह क्षेत्रों का क्षरण भी अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख पारिस्थितिक चिंता है। अतः यह अध्ययन क्षेत्र मरुस्थलीकरण के कारणों और प्रभावों को समझने हेतु उपयुक्त है, जहाँ प्राकृतिक कारणों (जैसे अल्प वर्षा, तेज हवाएँ, रेतीली मिट्टी) और मानवजनित हस्तक्षेप (अति-चराई, वनों की कटाई, जल दोहन) की भूमिका को स्पष्टता से देखा जा सकता है। 5. मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएँ (Processes of Desertification) राजस्थान में मरुस्थलीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक व मानवजनित कारकों की संयुक्त क्रिया से संचालित होती है। जलवायु की चरम परिस्थितियाँ, पारिस्थितिक असंतुलन, और भूमि संसाधनों का अवैज्ञानिक उपयोग इस प्रक्रिया को और तेज़ करते हैं। नीचे मरुस्थलीकरण की प्रमुख प्रक्रियाएँ विस्तार से वर्णित हैं: 5.1 मृदा अपरदन (Soil Erosion) राजस्थान के थार मरुस्थल एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण का सबसे प्राथमिक और तीव्र रूप है। • पवन अपरदन (Aeolian Erosion): तेज़ हवाएँ, विशेषकर मई से जुलाई के बीच, रेतीली भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह को उड़ाकर दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाती हैं। इससे मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है और भूमि की उत्पादकता घटती है। • जल अपरदन (Water Erosion): अल्पकालिक, लेकिन तीव्र वर्षा के दौरान सतही कटाव, गलीकरण (gullies) और रिल शीट इरोजन (sheet erosion) की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। विशेषतः अरावली की ढलानों और शुष्क पठारों में यह प्रक्रिया तीव्रता से कार्य करती है। उदाहरण: नागौर और पाली जिलों में वर्षा आधारित जल अपरदन से कई खेत बंजर भूमि में बदल चुके हैं। 5.2 वनस्पति आवरण का क्षय (Loss of Vegetation Cover) मरुस्थलीकरण की एक अन्य तीव्र प्रक्रिया वनस्पति आवरण का ह्रास है। • अत्यधिक चराई (Overgrazing): चरागाह भूमि का अत्यधिक उपयोग, विशेषकर ऊँट, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं द्वारा, भूमि को उजाड़ बना देता है। • वनों की कटाई: ईंधन की आवश्यकता, कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण वनस्पति क्षेत्र तेजी से घटा है, जिससे जलवायु संतुलन व मृदा स्थायित्व दोनों प्रभावित हुए हैं। उदाहरण: जोधपुर और बाड़मेर जिलों में ओरण और गऊचार भूमि पर अतिक्रमण के कारण जैव विविधता में भारी गिरावट आई है। 5.3 जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रवृत्तियाँ राजस्थान में स्थानीय स्तर पर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। • वर्षा की अनिश्चितता: राज्य के अधिकांश भागों में वर्षा का मानक विचलन 40% से अधिक है, जिससे वर्षा अनुमानित नहीं रहती और सिंचाई व फसल चक्र प्रभावित होते हैं। • तापमान में वृद्धि: पिछले दो दशकों में औसत तापमान में 1.2°C तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ती है और जल स्रोत तेजी से सूखते हैं। • सूखा घटनाओं की आवृत्ति: सूखे की पुनरावृत्ति दर अब पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। सांख्यिकीय साक्ष्य: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राजस्थान में 1901–2020 के बीच औसत वार्षिक वर्षा में 6.5% की गिरावट देखी गई है। 5.4 भूमिगत जल स्तर का क्षय (Declining Groundwater Levels) जल संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग मरुस्थलीकरण को गति देता है। • ट्यूबवेल सिंचाई का अत्यधिक उपयोग: विशेषतः नागौर, झुंझुनूं और अलवर जैसे क्षेत्रों में, किसानों द्वारा गहरे ट्यूबवेलों के माध्यम से जल निकासी के कारण भूजल स्तर हर वर्ष औसतन 0.5 से 1.0 मीटर तक गिर रहा है। • भूजल पुनर्भरण की कमी: जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण और वर्षा जल संचयन की उपेक्षा भूजल स्तर की पुनर्प्राप्ति को बाधित करते हैं। उदाहरण: सीकर जिले में 1990 के दशक में जो भूजल स्तर 25 मीटर था, वह अब 80 मीटर से अधिक हो गया है। 5.5 भूमि का अपर्याप्त उपयोग (Unsustainable Land Use) भूमि संसाधनों का अनियंत्रित और अवैज्ञानिक उपयोग मरुस्थलीकरण का आधार बनता है: • एकल फसल प्रणाली (Monocropping): एक ही प्रकार की फसल को बार-बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और भूमि बंजर हो जाती है। • रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग: यह मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और जैविक पदार्थों की मात्रा को नष्ट करता है। • जंगल और चारागाह भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन: इससे न केवल भूमि थकावट होती है बल्कि पारिस्थितिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है। उदाहरण: चूरू और झुंझुनूं जिलों में 2001–2021 के बीच चारागाह भूमि में 32% की गिरावट दर्ज की गई है (ISRO, 2021)। इन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से राजस्थान का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है। यह न केवल पर्यावरणीय संकट है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गंभीर चुनौती है। 6. मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण (Major Causes of Desertification) राजस्थान में मरुस्थलीकरण के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित दोनों प्रकार के कारण सक्रिय हैं। ये कारण एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए भूमि की गुणवत्ता को धीरे-धीरे नष्ट करते हैं, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। 6.1 प्राकृतिक कारण (Natural Causes) 1. अल्प वर्षा एवं असमान वितरण: राजस्थान के अधिकांश जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 500 मिमी के बीच होती है, जो देश के औसत से बहुत कम है। साथ ही, यह वर्षा स्थानिक और कालिक रूप से अत्यंत असमान होती है। वर्षा की यह अनिश्चितता भूमि की नमी को बनाए रखने में असफल होती है। 2. उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण दर: गर्मियों में तापमान 45–50°C तक पहुँच जाता है, जिससे मृदा में नमी की भारी कमी हो जाती है। वाष्पीकरण की दर वर्ष भर अत्यधिक बनी रहती है। 3. रेतीली और ढीली संरचना वाली मृदा: थार क्षेत्र की रेतयुक्त मृदा जल धारण क्षमता में कमज़ोर होती है। ये मृदाएँ पवन अपरदन के प्रति संवेदनशील होती हैं। 4. स्थलाकृति और प्राकृतिक ढाल: अरावली के आसपास की ढालदार भूमि पर वर्षा जल का बहाव तेज होता है, जिससे शीट इरोजन और गलीकरण की घटनाएँ अधिक होती हैं। 6.2 मानवजनित कारण (Anthropogenic Causes) 1. अत्यधिक पशुधन दबाव और चराई: राजस्थान में पशुधन घनत्व भारत के औसत से अधिक है। अत्यधिक चराई से चारागाह भूमि नष्ट होती है और जैवविविधता में गिरावट आती है। इससे मृदा की सतह असुरक्षित हो जाती है और वह तेजी से उड़ने लगती है। 2. वनों की अवैध कटाई और जैव आवरण की क्षति: ग्रामीण ईंधन की ज़रूरत, कृषि विस्तार और अवैध वनोत्पादन ने हरे आवरण को कम किया है। इससे भूमि पर तापमान का प्रभाव बढ़ता है और मृदा क्षरण की प्रक्रिया तेज होती है। 3. कृषि भूमि पर अतिक्रमण और शहरीकरण: खेतों और चारागाह भूमि पर आवासीय कॉलोनियाँ, सड़कें और औद्योगिक इकाइयाँ बनने से भूमि की जैव उत्पादकता नष्ट होती है। भूमि उपयोग में यह असंतुलन स्थायी मरुस्थलीकरण को जन्म देता है। 4. जल संसाधनों का अनियंत्रित दोहन: ट्यूबवेल, बोरवेल और अन्य गहरे जल निकासी साधनों के अत्यधिक प्रयोग से भूजल स्तर तेजी से गिरता है। भूजल की अनुपलब्धता से हरित भूमि धीरे-धीरे बंजर में बदल जाती है। विशेष उल्लेख: ISRO (2021) के अनुसार, राजस्थान का लगभग 62% क्षेत्र किसी न किसी रूप में मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जिसमें मानवजनित गतिविधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 7. मरुस्थलीकरण के प्रभाव (Impacts of Desertification) मरुस्थलीकरण के प्रभाव बहुआयामी होते हैं जो न केवल पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढाँचे को भी कमजोर करते हैं। • भूमि की उत्पादकता में गिरावट: बंजर होती ज़मीनों से उपज में निरंतर गिरावट आती है। रेत के फैलाव, मृदा क्षरण और पोषक तत्वों की कमी के कारण किसान खेती छोड़ने को विवश हो जाते हैं। • खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव: कृषि उत्पादकता घटने से खाद्यान्न की उपलब्धता कम होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ जाती है। • जल स्रोतों का क्षय और जलवायु कठोरता: मरुस्थलीकरण के क्षेत्रों में तालाब, कुएँ और अन्य जल स्रोत या तो सूख जाते हैं या खारे हो जाते हैं। इससे स्थानीय जलवायु और भी कठोर बन जाती है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। • आजीविका साधनों की समाप्ति और पलायन: पशुपालन, कृषि, चारागाह आधारित व्यवसाय और पारंपरिक आजीविकाएँ समाप्त होने लगती हैं। इससे लोगों को रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। • जैव विविधता और पारिस्थितिक असंतुलन: चरागाहों और वनों के नष्ट होने से पशु-पक्षियों की प्रजातियाँ लुप्त होने लगती हैं। खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन टूटता है। 8. मरुस्थलीकरण नियंत्रण उपाय (Desertification Control Measures) मरुस्थलीकरण एक बहुआयामी पर्यावरणीय संकट है, जिसकी रोकथाम के लिए केवल एक समाधान पर्याप्त नहीं हो सकता। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्ध-शुष्क राज्य में इसके नियंत्रण हेतु समन्वित, क्षेत्र-विशेष और जनभागीदारी पर आधारित रणनीतियाँ अपनाना अनिवार्य है। मरुस्थलीकरण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय प्रभावी माने जाते हैं: 8.1 स्थायी भूमि उपयोग योजना (Sustainable Land Use Planning) • भूमि की क्षमता आधारित उपयोग नीति बनाकर कृषि, वानिकी और चरागाहों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण किया जाना चाहिए। • कृषि भूमि पर नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। • भूमि उपयोग परिवर्तन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु GIS और रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग बढ़ाया जाए। 8.2 वनावरण पुनर्स्थापना (Reforestation and Afforestation) • स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय पेड़ और झाड़ियों जैसे बबूल, खेजड़ी, केर, बेर आदि का बड़े पैमाने पर रोपण किया जाना चाहिए। • वन संरक्षण अधिनियम के तहत ओरण, गोचर और ग्राम वनों का पुनरुद्धार किया जाए। • रेतीले टिब्बों पर घासों की पट्टी (Grass Strip Plantation) लगाकर रेत के उड़ाव को रोका जा सकता है। 8.3 जल संसाधनों का संरक्षण (Water Resource Management) • वर्षा जल संचयन को प्रत्येक गाँव, विद्यालय, भवन और खेत पर अनिवार्य किया जाना चाहिए। • पारंपरिक जल संरचनाएँ जैसे जोहड़, टांके, नाड़ी, खाल, आदि का पुनरुद्धार किया जाए। • भूजल पुनर्भरण हेतु चेक डैम, परकोलेशन टैंक, जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना को स्थानीय निकायों से जोड़ा जाए। 8.4 चारागाह प्रबंधन (Pastureland Management) • गोचर और चरागाह भूमि पर सीमांकन, पौधरोपण और चराई प्रबंधन किया जाना चाहिए। • घूर्णन चराई (Rotational Grazing) की प्रणाली अपनाई जाए ताकि भूमि को पुनर्जीवित होने का अवसर मिले। • समुदाय आधारित पशु संख्या नियंत्रण योजना चलाई जाए। 8.5 मृदा संरक्षण तकनीकें (Soil Conservation Techniques) • टिब्बों पर फेंसिंग और घास की पट्टियाँ लगाकर हवा से उड़ने वाली मिट्टी को रोका जा सकता है। • कॉन्टूर बंडिंग, स्टोन चेक, झाड़ियों की बाधाएँ जैसे भौतिक उपाय अपनाने से जल और मृदा का क्षरण रुकता है। • मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि हेतु हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, और बायोमास का उपयोग बढ़ाया जाए। 8.6 जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी (Awareness and Community Participation) • स्थानीय समाज को पर्यावरण शिक्षा और मृदा-पानी संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है। • महिला स्वयं सहायता समूह, विद्यालयों, और ग्राम सभाओं को संरक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। • जनसुनवाई और ग्रामीण कार्यशालाओं के माध्यम से नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 8.7 नीति और प्रशासनिक समर्थन (Policy and Institutional Support) • मरुस्थलीकरण रोधी कार्यों को राज्य कृषि नीति, भूमि उपयोग नीति और जल नीति से जोड़ा जाए। • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एकीकृत मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम (IDCP) जैसे कार्यक्रमों को फिर से सक्रिय किया जाए। • ISRO, NIH, CAZRI जैसे अनुसंधान संस्थानों के साथ तालमेल बढ़ाकर विज्ञान आधारित समाधान लागू किए जाएँ। मरुस्थलीकरण का प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। राजस्थान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। 9. सुझाव (Suggestions) राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में मरुस्थलीकरण का समाधान केवल तकनीकी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समग्र, बहु-स्तरीय और स्थानीय सशक्तिकरण पर आधारित रणनीतियों की आवश्यकता है। निम्नलिखित सुझाव इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं: 9.1 क्षेत्रीय भूमि उपयोग नियोजन • प्रत्येक ज़िले या ब्लॉक स्तर पर भूमि उपयोग क्षमता का वैज्ञानिक आकलन कर उपयुक्त भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए जाएँ। • मरुस्थलीकरण संभावित क्षेत्रों को "इकोलॉजिकल जोन" घोषित कर वहाँ असंवेदनशील भूमि उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। 9.2 पारंपरिक जल एवं भूमि प्रबंधन प्रणाली का पुनरुद्धार • बावड़ी, जोहड़, टांके, नाड़ी जैसे पारंपरिक जल संग्रहण साधनों का वैज्ञानिक पुनरुद्धार किया जाए। • स्थानीय समुदायों के सहयोग से गोचर भूमि, ओरण व परंपरागत चारागाह क्षेत्रों का पुनर्स्थापन किया जाए। 9.3 पौधारोपण अभियान और हरित पट्टियाँ • मरुस्थल के किनारे तथा टिब्बों पर घास-पट्टी और कांटेदार झाड़ियों की हरित पट्टियाँ बनाई जाएँ। • शुष्क क्षेत्रीय प्रजातियों जैसे खेजड़ी, बबूल, बेर आदि के वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिले। 9.4 सिंचाई में सुधार और जल संरक्षण तकनीकें • टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली को प्रोत्साहित कर जल अपव्यय को रोका जाए। • फसल विविधीकरण को अपनाकर जल-गहन फसलों के स्थान पर मौसमी और सूखा सहनशील फसलों की खेती की जाए। 9.5 जनशिक्षा और जनभागीदारी • ग्राम स्तर पर जल और मृदा संरक्षण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। • विद्यालय पाठ्यक्रमों में मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल किया जाए। 9.6 अनुसंधान एवं तकनीकी सहयोग • ICAR, CAZRI, और ISRO जैसे अनुसंधान संस्थानों से मरुस्थलीकरण से संबंधित डेटा और तकनीक साझा की जाए। • रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से भूमि की स्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाए। 9.7 प्रशासनिक और वित्तीय उपाय • मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यों हेतु स्थायी वित्तीय कोष की स्थापना हो। • स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतें, नगर पालिकाएँ) को भूमि संरक्षण योजनाओं में बजट और अधिकार दिए जाएँ। 9.8 सामुदायिक आधारित आजीविका योजनाएँ • मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में गौशालाओं, वन-उत्पादों, और डेयरी आधारित आजीविका को बढ़ावा दिया जाए। • ग्रामीण महिलाओं को पौध नर्सरी, कंपोस्ट उत्पादन, और स्थानीय जल संरक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रशिक्षित किया जाए। सुझावों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें नीति, विज्ञान, परंपरा और जनता—चारों की सहभागिता से लागू किया जाए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को केवल संकट नहीं, बल्कि सतत विकास हेतु अवसर के रूप में देखा जाए, जहाँ स्थानीय ज्ञान और आधुनिक नवाचार साथ मिलकर पर्यावरणीय संतुलन को पुनःस्थापित कर सकते हैं। 10. निष्कर्ष (Conclusion) राजस्थान का भौगोलिक और जलवायु परिदृश्य अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जहाँ मरुस्थलीकरण एक दीर्घकालिक और बहुआयामी संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि मरुस्थलीकरण मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानवजनित गतिविधियों, भूमि के अति-दोहन, असंतुलित जल प्रबंधन, वनविनाश, और भूमि उपयोग में असंगतियों का भी प्रतिफल है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी प्रभावित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता, आजीविका संकट, खाद्य असुरक्षा और जनसंख्या विस्थापन जैसी स्थितियों को जन्म देता है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर जैसे जिलों में यह संकट और भी गहराता जा रहा है। इस अध्ययन में यह भी उजागर हुआ है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया स्थानिक रूप से भिन्न है—कुछ क्षेत्रों में यह तेज़ है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह नियंत्रण में है। इसलिए, समाधान भी एकरूप नहीं हो सकते। स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं, समाज की सांस्कृतिक संरचना और आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट और बहुस्तरीय रणनीतियों की आवश्यकता है। यह भी देखा गया कि राजस्थान में अनेक पारंपरिक उपाय पहले से मौजूद हैं—जैसे जोहड़, खाल, ओरण, गोचर इत्यादि—जिन्हें वैज्ञानिक तकनीकों के साथ जोड़कर अत्यंत प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को यदि संसाधन और अधिकार मिलें, तो वे मरुस्थलीकरण से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अंततः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि सरकार, नीति निर्माता, वैज्ञानिक समुदाय, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक एक साझा मंच पर आकर कार्य करें, तो न केवल मरुस्थलीकरण की गति को रोका जा सकता है, बल्कि राजस्थान के पर्यावरणीय परिदृश्य को स्थिरता, उत्पादकता और सततता की दिशा में पुनः मोड़ा जा सकता है। मरुस्थलीकरण नियंत्रण अब केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास का आधार बन चुका है। यही समय है जब राजस्थान को एक जलवायु-संवेदनशील, मृदा-प्रवंधित और सामुदायिक-सशक्त राज्य के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए। 11. संदर्भ सूची 1. Government of India. (2020). Desertification and Land Degradation Atlas of India. Space Applications Centre, ISRO. pp. 46–61, 98–105. 2. Rajasthan State Action Plan on Climate Change. (2019). Government of Rajasthan. pp. 28–42. 3. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI). (2016). Land Degradation in Western Rajasthan. Jodhpur. pp. 14–37, 89–93. 4. National Remote Sensing Centre. (2018). Wasteland Mapping of Rajasthan. ISRO, Hyderabad. pp. 31–48. 5. Singh, R.P. & Sharma, M. (2017). “Desertification and Land Use in Thar Desert: A Case Study.” Journal of Arid Environments, Vol. 141, pp. 122–134. 6. UNEP. (2015). Global Assessment of Desertification. United Nations Environment Programme. pp. 72–88. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
| Cite This | राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएँ, कारण और नियंत्रण उपाय: एक पर्यावरणीय भूगोलीय अध्ययन - Shipra Vyas - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

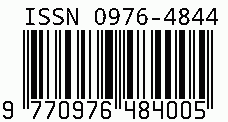
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

