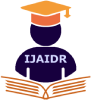
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
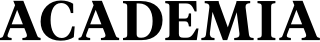













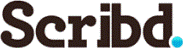




प्रेमचंद की कहानियों में नारी जीवन का साहित्यिक अवलोकन
| Author(s) | LALA RAM |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | हिंदी कथा-साहित्य के विकास में मुंशी प्रेमचंद का योगदान अद्वितीय है। उन्हें आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास का पितामह माना जाता है। उन्होंने जिस यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली, वह केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन थी, जिसमें उन्होंने समाज के उपेक्षित, शोषित, पीड़ित और हाशिए पर खड़े वर्गों को न केवल स्वर दिया, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत भी किया। इस सामाजिक यथार्थ की सबसे सशक्त और संवेदनशील अभिव्यक्ति उनके स्त्री-पात्रों में दिखाई देती है। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय नारी जीवन के विविध पक्षों को अत्यंत आत्मीयता, सूक्ष्मता और संवेदना के साथ उद्घाटित करता है। वह नारी को एक सामाजिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत, भावनाशील और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में चित्रित करते हैं। उनके लिए स्त्री केवल गृहस्थी की धुरी या करुणा की पात्र नहीं, बल्कि संघर्षशील चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित नारी पात्र बहुधा ग्रामीण, निर्धन और निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन उनमें साहस, विवेक और सहनशीलता का अद्भुत समन्वय होता है। वे पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़ियों से टकराती हैं, अत्याचार और अन्याय का विरोध करती हैं, और कई बार मौन संघर्ष के माध्यम से बदलाव की प्रेरणा देती हैं। ‘बड़े घर की बेटी’ की अनारकली, ‘माँ’ की निरुपाय वृद्धा, ‘ठाकुर का कुआँ’ की गंगी, और ‘स्त्री और पुरुष’ की आत्मसम्मानी नायिका—ये सभी पात्र प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि की विविधता और सामाजिक गहराई को दर्शाते हैं। स्त्री जीवन पर प्रेमचंद का दृष्टिकोण न तो केवल दया और करुणा से संचालित है और न ही कट्टर आदर्शवाद से। वह स्त्री की समस्याओं को उसके सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में रखते हुए उसका यथार्थ चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों में स्त्री के संघर्ष, उसकी अस्मिता की खोज, उसकी चुप्पी और विद्रोह—सब कुछ अत्यंत मार्मिक और प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत होता है। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जब अधिकांश साहित्यकार स्त्री को केवल प्रेम, सौंदर्य और त्याग की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, तब प्रेमचंद ने उसे विचारशील, संघर्षशील और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह दृष्टिकोण अपने समय में क्रांतिकारी था, और इसने हिंदी साहित्य में नारी-विमर्श की नींव रखने का कार्य किया। प्रेमचंद की लेखनी नारी के प्रति केवल भावुक करुणा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का उपकरण बनती है। वे चाहते थे कि स्त्री भी पुरुष के समान समाज में सक्रिय भूमिका निभाए वह केवल समर्पण न करे, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करे, अन्याय का प्रतिरोध करे और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करे। इस शोध-पत्र के माध्यम से प्रेमचंद की कहानियों में नारी जीवन की विविध छवियों, संघर्षों, सामाजिक स्थितियों और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि आज के नारी विमर्श के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक और प्रेरक है। 2. शोध उद्देश्य (Objectives of the Study) यह शोध-पत्र प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित नारी जीवन का साहित्यिक और सामाजिक विश्लेषण करता है। इसके माध्यम से नारी पात्रों के चरित्र, संघर्ष, सामाजिक संदर्भ और आत्मचेतना को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 1. प्रेमचंद की कहानियों में नारी पात्रों के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण करना: इस उद्देश्य के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा रचित विभिन्न कहानियों में नारी पात्रों की भूमिका, उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक व्यवहार और उनकी आंतरिक शक्ति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन यह जानने का प्रयास करेगा कि प्रेमचंद की नायिकाएँ केवल सहनशील पात्र नहीं, बल्कि सामाजिक रूपांतरण की प्रेरणा भी हैं। 2. प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री जीवन की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझना: यह उद्देश्य प्रेमचंद की कहानियों में प्रस्तुत उस समाज की पड़ताल करता है जिसमें स्त्री जीवन अभिव्यक्त हुआ है। इसमें यह देखा जाएगा कि कैसे जातीय, वर्गीय, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, और प्रेमचंद ने इन स्थितियों को किस रूप में चित्रित किया है। 3. प्रेमचंद की दृष्टि में नारी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अधिकारों की स्थिति को पहचानना: इस बिंदु के अंतर्गत यह विश्लेषण किया जाएगा कि प्रेमचंद नारी को कितनी स्वतंत्र और अधिकार सम्पन्न मानते हैं। उनकी कहानियों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की आकांक्षा रखने वाली स्त्रियाँ किस प्रकार पितृसत्ता से संघर्ष करती हैं और कैसे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। 4. उनकी कहानियों में नारी विमर्श के आरंभिक स्वरूप की पहचान करना: यह उद्देश्य प्रेमचंद के साहित्य में नारी विमर्श के प्रारंभिक स्वरूप और प्रवृत्तियों को उजागर करता है। विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कैसे उनके लेखन में स्त्री विषयक चिंतन केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेतक भी बनता है। 3. शोध पद्धति (Research Methodology) यह शोध एक साहित्यिक और गुणात्मक (Qualitative) विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य प्रेमचंद की कहानियों में नारी जीवन के विविध पक्षों का सम्यक रूप से अन्वेषण करना है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) एवं समीक्षात्मक (Analytical) दृष्टिकोण को अपनाया गया है। मुख्य आधार और तकनीकें: 1. प्राथमिक स्रोतों का चयन: शोध के लिए प्रेमचंद की चयनित कहानियाँ जैसे — ‘सद्गति’, ‘कफन’, ‘स्त्री और पुरुष’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘माँ’, ‘ठाकुर का कुआँ’, ‘गबन’ आदि को मूल पाठ के रूप में लिया गया है। इन रचनाओं का गहन पाठ विश्लेषण (Close Reading) कर पात्रों, घटनाओं, संवादों और कथावाचन की शैली के माध्यम से स्त्री जीवन की संवेदना और यथार्थ को समझा गया है। 2. द्वितीयक स्रोतों का परिशीलन: शोध के संदर्भ में आलोचकीय ग्रंथ, शोध-पत्र, स्त्री विमर्श से संबंधित विद्वानों के लेख, और समकालीन सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन—इन सभी का सहायक रूप में उपयोग किया गया है। इसमें रामविलास शर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, सुधा अरोड़ा और अन्य आलोचकों के विचारों को संदर्भित किया गया है। 3. नारीवादी साहित्यिक दृष्टिकोण (Feminist Literary Perspective): अध्ययन में नारीवाद की प्रमुख अवधारणाओं जैसे पितृसत्ता, स्त्री अस्मिता, सामाजिक उत्पीड़न, आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध चेतना को आधार बनाकर कहानियों का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण भारतीय सन्दर्भ में विकसित नारी विमर्श के आलोक में किया गया है। 4. सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन: प्रेमचंद की कहानियाँ जिन सामाजिक परिवेशों को प्रतिबिंबित करती हैं, उनका मूल्यांकन तत्कालीन भारतीय समाज की जातिगत, वर्गीय, आर्थिक और लिंग-आधारित संरचनाओं के संदर्भ में किया गया है। 5. गुणात्मक शोध विधियाँ (Qualitative Techniques): शोध में मात्रात्मक आँकड़ों के स्थान पर व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें: o Textual Analysis (पाठ विश्लेषण) o Thematic Analysis (विषयवस्तु आधारित विश्लेषण) o Character Study (पात्र विश्लेषण) o Comparative Reflection (तुलनात्मक दृष्टिकोण) सम्मिलित हैं। शोध क्षेत्र और सीमा (Scope and Limitation) यह अध्ययन प्रेमचंद की कहानियों तक सीमित है, विशेषकर वे कहानियाँ जिनमें नारी पात्रों की उपस्थिति प्रमुख है। इसमें उपन्यासों की अपेक्षा केवल कहानियों को ही विश्लेषण का आधार बनाया गया है। शोध में आधुनिक स्त्रीवादी लेखन से तुलना का प्रयास सीमित है, और इसका फोकस प्रेमचंद की नारी दृष्टि के ऐतिहासिक और साहित्यिक मर्म को उजागर करने पर केंद्रित है। 4. प्रेमचंद की नारी दृष्टि प्रेमचंद की नारी दृष्टि भारतीय समाज के उस ऐतिहासिक मोड़ पर विकसित हुई जब स्त्री की सामाजिक स्थिति असमानता, शोषण और पितृसत्ता के कठोर घेरे में थी। उस युग में स्त्री को केवल एक घरेलू इकाई, त्याग और सेवा की मूर्ति तथा पुरुष की छाया के रूप में देखा जाता था। प्रेमचंद ने इस दृष्टिकोण को नकारते हुए स्त्री को एक स्वतंत्र, सजग, आत्मसम्मानी और विचारशील प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों में नारी केवल कोमलता या शील की प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष, चेतना और परिवर्तन की वाहिका है। प्रेमचंद की नारी दृष्टि करुणा पर आधारित जरूर है, किंतु यह करुणा एक सक्रिय सामाजिक हस्तक्षेप का रूप लेती है। वह नारी को दया की पात्र मानकर केवल सहानुभूति नहीं जताते, बल्कि उसके पक्ष में खड़े होते हैं और उसे सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। 1. नारी: सहनशीलता से प्रतिरोध तक: प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री का रूप बहुधा अत्याचार सहने वाली लेकिन अंततः प्रतिरोध करने वाली इकाई के रूप में सामने आता है। ‘बड़े घर की बेटी’ की अनारकली इसका आदर्श उदाहरण है, जो सामंती परिवेश में रहते हुए भी आत्मसम्मान के साथ निर्णय लेती है। वह अपने पति और परिवार के बीच मध्यस्थता करते हुए न केवल स्त्री विवेक का परिचय देती है, बल्कि पारिवारिक संतुलन को भी बनाए रखती है। 2. सामाजिक यथार्थ की संवाहिका: प्रेमचंद स्त्री को समाज के यथार्थ से अलग नहीं करते। उनके लिए स्त्री समाज की सच्चाइयों की प्रतिनिधि है—वह कहीं ग़रीबी की मार झेलती हुई कृषक स्त्री है (‘ठाकुर का कुआँ’), तो कहीं पुत्रमोह में फंसी हुई एक त्यागमयी माँ है (‘माँ’)। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि स्त्री जीवन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबावों से भी गहरे रूप में प्रभावित है। 3. स्त्री चेतना का उभार: प्रेमचंद की कहानियों में नारी चेतना का बीज दिखाई देता है, जो उस समय के समाज में अभूतपूर्व था। ‘स्त्री और पुरुष’ जैसी कहानियाँ इस चेतना को शब्द देती हैं, जहाँ नायिका अपने पति की स्वेच्छाचारिता का प्रतिरोध करती है और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानती है। यह नारी केवल प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग है और पितृसत्तात्मक व्यवहार को अस्वीकार करती है। 4. नारी और नैतिकता का पुनर्पाठ: प्रेमचंद की दृष्टि में स्त्री नैतिकता की मूर्ति नहीं, बल्कि एक मनुष्य है—जिसमें इच्छाएँ भी हैं, विवेक भी, और संघर्ष की क्षमता भी। वह नैतिकता की परंपरागत परिभाषाओं को चुनौती देती है। ‘गबन’ की जालपा एक आधुनिक नारी है जो गहनों के प्रति आकर्षण रखती है, लेकिन जब उसे सच्चाई का आभास होता है, तो वह अपने पति के अपराध को स्वीकार नहीं करती और उसे आत्मस्वीकृति की ओर प्रेरित करती है। यह प्रेमचंद की उस नारी दृष्टि को उजागर करता है, जो स्त्री को न तो देवता बनाती है, न दासी—बल्कि एक जागरूक, विवेकशील, नैतिक रूप से सक्रिय इकाई मानती है। 5. नारी मुक्ति का सामाजिक आधार: प्रेमचंद यह मानते थे कि नारी मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए उनकी कहानियाँ केवल स्त्रियों को नहीं, समाज को भी संबोधित करती हैं। वे पुरुषों, परंपराओं, धर्म, रीति-नीति और सामाजिक संरचना को प्रश्नांकित करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें नारीवादी आलोचकों के लिए प्रासंगिक बनाता है। 5. स्त्री जीवन के विविध रूप: प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय स्त्री जीवन के बहुरूपी आयामों की एक सजीव और यथार्थपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती हैं। उनके कथा-साहित्य में स्त्री कभी एक शोषित पीड़िता है, कभी आत्मसमर्पित माँ, कभी साहसी विद्रोहिणी तो कभी चुपचाप जूझती हुई परंतु भीतर से दृढ़ नारी। प्रेमचंद की नायिकाएँ न केवल सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि वे उन परिवर्तनों की संभावनाओं को भी इंगित करती हैं जो स्त्री की भूमिका को एक निष्क्रिय इकाई से एक सक्रिय सामाजिक इकाई की ओर ले जाती हैं। 1. संकटग्रस्त ग्रामीण स्त्री: मौन प्रतिरोध का स्वरूप: प्रेमचंद की कहानी ‘ठाकुर का कुआँ’ में गंगी एक निम्नवर्गीय दलित स्त्री है, जो अपने बीमार पति के लिए ठाकुरों के कुएँ से पानी भरने जाती है, जबकि समाज में उसकी जाति को वहाँ से पानी लेना वर्जित है। यह कहानी केवल जातिगत भेदभाव नहीं, बल्कि स्त्री के साहस और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ मौन प्रतिरोध की कथा भी है। गंगी की चुपचाप की गई यह कार्यवाही प्रेमचंद की उस स्त्री को प्रस्तुत करती है जो बिना शोर किए बदलाव की नींव रखती है। यह पात्र सामाजिक अन्याय के विरुद्ध स्त्री की आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को उजागर करता है। 2. मातृत्व की करुणा और विडंबना: सहिष्णुता की चरम सीमा: कहानी ‘माँ’ एक वृद्धा के त्याग और मातृत्व की अमरता को केंद्र में रखती है। पुत्रवधू और बेटे द्वारा उपेक्षित किए जाने के बावजूद वह माँ न केवल उन्हें क्षमा करती है, बल्कि उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करती है। यह पात्र भारतीय मातृत्व की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ स्त्री का प्रेम और क्षमा समाज की हर क्रूरता को पार कर जाता है। प्रेमचंद इस कथा के माध्यम से यह दिखाते हैं कि भारतीय नारी केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि अपार सहिष्णुता की मूर्ति भी है। 3. शोषित और उपेक्षित नारी: पीड़ा की गहराई में बसी अस्मिता: ‘सद्गति’ और ‘कफन’ जैसी कहानियाँ स्त्री जीवन की उस भीषण सच्चाई को सामने लाती हैं, जो गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक शोषण के बीच पिसती रहती है। ‘सद्गति’ में दुखी की पत्नी अपने पति की मृत्यु पर समाज द्वारा ठुकराई गई है और उसका दु:ख दोहरा है—पति का गम और जातिगत अपमान। वहीं ‘कफन’ में घीसू और माधव की मृत पत्नी/बहू केवल एक उपेक्षित स्त्री नहीं, बल्कि पुरुष की स्वार्थपरता और स्त्री की अवहेलना का प्रतीक बन जाती है। इन कहानियों की स्त्रियाँ न केवल शोषण का शिकार हैं, बल्कि उनके माध्यम से प्रेमचंद उस समाज की अमानवीयता पर प्रश्नचिह्न भी लगाते हैं जो स्त्री को केवल 'उपयोग की वस्तु' मानता है। 4. नारी का विद्रोही स्वर: आत्मसम्मान और अस्मिता की पुकार: प्रेमचंद की कहानी ‘स्त्री और पुरुष’ उस स्त्री की कथा है जो पति की अन्य स्त्रियों के साथ संलग्नता को सहन नहीं करती और प्रतिकार करती है। यह नारी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है और स्पष्ट करती है कि प्रेम और विवाह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक निष्ठा की अपेक्षा करते हैं। यह कहानी प्रेमचंद की उस आधुनिक दृष्टि को स्पष्ट करती है, जहाँ नारी को सजग, स्वतंत्र और निर्णय लेने योग्य माना गया है। 1. यह विद्रोही स्वर प्रेमचंद की नारी दृष्टि को केवल सहिष्णुता और करुणा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ स्त्री अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ी होती है। यह प्रेमचंद के स्त्री विमर्श में आधुनिक चेतना और अधिकारबोध का प्रारंभिक संकेतक है। प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री जीवन के ये विविध रूप न केवल उनकी साहित्यिक प्रतिभा का परिचायक हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि उन्होंने स्त्री को केवल पीड़िता नहीं, बल्कि समाज के परिवर्तन की शक्ति के रूप में देखा। प्रेमचंद की स्त्रियाँ अपनी चुप्पी में भी मुखर हैं, अपने त्याग में भी विद्रोही हैं और अपने संघर्ष में भी गरिमा से भरपूर हैं। उनका यह स्त्री चित्रण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यद्यपि प्रेमचंद का साहित्य 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रचा गया था, जब भारतीय समाज परंपरागत रूढ़ियों, धार्मिक व सामाजिक बंधनों और पितृसत्ता के प्रभाव में जकड़ा हुआ था, फिर भी उनकी कहानियों में नारी के संबंध में जो दृष्टिकोण सामने आता है, वह अत्यंत प्रगतिशील, मानवीय और विमर्शात्मक है। प्रेमचंद की नारी केवल एक करुणा की पात्र नहीं, बल्कि समानता, आत्मसम्मान और स्वायत्तता की जिज्ञासु आकांक्षा है। प्रेमचंद ने नारी को सामाजिक संस्थाओं और परिवार के पारंपरिक ढांचों में बंद एक निष्क्रिय इकाई के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे बदलते समाज की सशक्त आवाज़, प्रश्न और संघर्ष की प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उनकी नायिकाएँ घरेलू भूमिका निभाते हुए भी सामाजिक अन्याय के प्रति सजग रहती हैं और अनेक बार विद्रोह या मौन प्रतिकार के माध्यम से स्त्री चेतना के बीज बोती हैं। ‘स्त्री और पुरुष’ की नायिका जब पति की बहुविवाहप्रिय प्रवृत्ति का विरोध करती है, तो वह उस युग में स्त्री मुक्ति का स्वर बन जाती है जहाँ स्त्री की निष्ठा को तो अनिवार्य माना जाता था, परंतु पुरुष के लिए स्वतंत्रता स्वाभाविक अधिकार समझी जाती थी। इसी प्रकार ‘ठाकुर का कुआँ’ की गंगी जातिगत और लैंगिक दोहरे शोषण के बावजूद साहसी कदम उठाती है और व्यवस्था को चुनौती देती है। इन कहानियों में प्रेमचंद स्त्री को किसी वाद की दासी नहीं बनाते, बल्कि एक चिंतनशील, संघर्षशील और बदलाव की वाहक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका स्त्री विमर्श पश्चिमी नारीवाद से भिन्न, किंतु उससे कम प्रभावशाली नहीं है। यह भारतीय यथार्थ से जुड़ा एक मौलिक स्त्री दृष्टिकोण है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए नारी को केंद्र में लाता है। 7. सामाजिक आलोचना और नारी मुक्ति (Social Critique and Women's Liberation) प्रेमचंद का साहित्य केवल कहानी नहीं कहता, बल्कि समाज से संवाद करता है—विशेषतः उस समाज से जिसमें स्त्री की भूमिका सीमित, श्रम अदृश्य और अस्तित्व गौण बना दिया गया है। उनकी नारी पात्रें न केवल जीवन के विविध कष्टों को सहती हैं, बल्कि उन मूल्यों और ढाँचों पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं जो स्त्री को द्वितीयक और पराश्रित मानते हैं। उनकी कहानियाँ जैसे ‘माँ’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘कफन’, ‘गबन’ आदि में स्त्रियाँ जिस प्रकार मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं, वह केवल स्त्री की स्थिति का चित्रण नहीं, बल्कि समाज की उस नैतिक और वैचारिक दुर्बलता की कड़ी आलोचना है जो स्त्री श्रम और संवेदना को ‘कर्तव्य’ समझकर उसका मूल्यांकन नहीं करती। प्रेमचंद की नारी मुक्ति की संकल्पना न केवल व्यक्तिगत स्वाधीनता पर आधारित है, बल्कि वह सामाजिक पुनर्रचना की मांग करती है। वे स्पष्ट करते हैं कि स्त्री की मुक्ति केवल स्त्री का प्रश्न नहीं, बल्कि समाज के पुनर्गठन का एक अनिवार्य अंग है। उनकी लेखनी नारी को ‘गृहस्थी की शोभा’ के खांचे से निकालकर एक स्वतंत्र, विचारशील और निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में चित्रित करती है। इस दृष्टिकोण में प्रेमचंद आधुनिक नारी विमर्श के पूर्वज प्रतीत होते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक स्त्री को उसका सम्मान, अधिकार और अस्तित्व की स्वतंत्रता प्राप्त न हो। उनका साहित्य, विशेषकर कहानियाँ, एक प्रकार का ‘साहित्यिक प्रतिरोध’ (Literary Resistance) बन जाती हैं, जो स्त्री के पक्ष में खड़ी होती हैं। 8. निष्कर्ष (Conclusion) प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी साहित्य में केवल यथार्थवादी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता, मानवीय करुणा और विचारधारा की सशक्त अभिव्यक्ति भी हैं। विशेषतः उनके कथा-साहित्य में नारी जीवन का चित्रण एक ऐतिहासिक-सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ स्त्री को केवल भावना और त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि एक सोचने-समझने वाली, निर्णय लेने वाली, और अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली इकाई के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेमचंद ने नारी के माध्यम से पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत अन्याय, आर्थिक शोषण और सामाजिक रूढ़ियों को ललकारा है। उनकी कहानियों में नारी पात्र जिस सूक्ष्मता से अपने अधिकार, आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी के लिए संघर्ष करती हैं, वह न केवल उस युग के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि आज के समाज के लिए भी प्रेरणास्रोत है। उनकी नायिकाएँ जैसे गंगी, अनारकली, जालपा, सिलिया या स्त्री और पुरुष की विद्रोहिणी—ये सभी पात्र उस मौन प्रतिरोध की प्रतीक हैं जो संवेदनशीलता से शुरू होकर परिवर्तन की चेतना तक पहुँचता है। ये पात्र प्रश्न करती हैं, मार्ग चुनती हैं, और अपने विवेक से सामाजिक असंतुलन को संतुलन में बदलने का प्रयास करती हैं। प्रेमचंद की नारी दृष्टि में न तो अति भावुकतावाद है और न ही उग्र आदर्शवाद, बल्कि एक संतुलित, यथार्थवादी और परिवर्तनकामी दृष्टिकोण है, जो उन्हें आधुनिक नारी विमर्श के पूर्वगामी के रूप में स्थापित करता है। उनकी कहानियाँ यह दिखाती हैं कि नारी को उसकी भूमिका केवल 'गृहस्थी की धुरी' के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्रचना की प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज जब 21वीं सदी का समाज भी लैंगिक असमानता, स्त्री हिंसा और सामाजिक भेदभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, तब प्रेमचंद का साहित्य और अधिक प्रासंगिक हो उठता है। उनका स्त्री विषयक दृष्टिकोण हमें यह विचार करने को बाध्य करता है कि क्या आधुनिक समाज ने वास्तव में स्त्री को उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान किए हैं? अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि प्रेमचंद की कहानियाँ महज़ साहित्यिक धरोहर नहीं, बल्कि स्त्री जीवन के संघर्ष, चेतना और मुक्ति की यात्रा की साहित्यिक दस्तावेज़ हैं। वे आज भी हमें नारी के प्रश्नों को नए सिरे से सोचने, समझने और पुनर्परिभाषित करने की प्रेरणा देती हैं। 9. संदर्भ सूची (References) 1. प्रेमचंद, मुंशी. मानसरवर (भाग 1-8)। नई दिल्ली: लोकभारती प्रकाशन। 2. श्रीवास्तव, रामविलास. (2003). प्रेमचंद का कथा साहित्य। वाराणसी: नागरी प्रचारिणी सभा। 3. ओझा, गिरिराजशरण. (2010). प्रेमचंद और नारी चेतना। दिल्ली: साहित्य भवन। 4. देव, नागेन्द्र। (1995). हिंदी साहित्य का इतिहास। इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन। 5. Sharma, Sudhir Chandra. (2002). Premchand and the Changing World of Women in India. Economic and Political Weekly, Vol. 37(1), pp. 44-50. 6. Dalmia, Vasudha. (2007). The Nationalization of Hindu Traditions: Bharatendu Harishchandra and Nineteenth-Century Banaras. Oxford University Press. 7. Nehru, Krishna. (2014). Reading Women in Premchand’s Fiction. Journal of South Asian Literature, Vol. 26(3), pp. 112–129. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
| Cite This | प्रेमचंद की कहानियों में नारी जीवन का साहित्यिक अवलोकन - LALA RAM - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

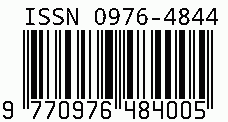
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

