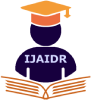
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
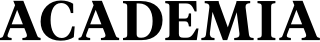













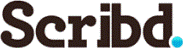




भारत जल-संकटग्रस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से समाधान और उपाय
| Author(s) | Ram Singh Jatav |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | जल न केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के संपूर्ण तंत्र का आधार है। कृषि, उद्योग, पशुपालन, ऊर्जा उत्पादन और घरेलू उपयोग — सभी क्षेत्रों में जल की केंद्रीय भूमिका है। किंतु वर्तमान में भारत एक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जो न केवल एक पर्यावरणीय चिंता है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी बन चुका है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता निरंतर घटती जा रही है; वर्ष 1951 में यह आंकड़ा जहाँ लगभग 5,177 घन मीटर था, वहीं 2020 तक यह घटकर लगभग 1,486 घन मीटर रह गया है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो निकट भविष्य में भारत "जल-संकटग्रस्त राष्ट्र" (Water-Stressed Country) की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वर्तमान जल संकट की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ मानवजनित कारण भी उतने ही उत्तरदायी हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से भारत का जल संकट एक विषम वर्षा वितरण, भौगोलिक असमानता, अनियमित मानसून, स्थलाकृति और भूमिगत जल संरचनाओं के असंतुलित उपयोग से जुड़ा हुआ है। वहीं, जनसंख्या वृद्धि, असंतुलित नगरीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा, जल-गहन फसलों की खेती, और अनुचित जल नीति के चलते यह संकट और अधिक गहराता जा रहा है। यह शोधपत्र जल संकट की समस्या को विशुद्ध भूगोलिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, जिसमें जल संसाधनों के वितरण, उपयोग, पुनर्भरण क्षमता, जलवायु प्रभाव और मानवीय हस्तक्षेप को समझते हुए समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें यह भी विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार भौगोलिक विविधताओं वाले भारत में स्थान विशेष की भौतिक और पारिस्थितिकीय स्थितियों को ध्यान में रखकर जल प्रबंधन रणनीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह शोध सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से भी जल संकट के प्रभावों को समझता है — जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की असमान पहुँच, कृषक समुदायों पर प्रभाव, महिलाओं और बच्चों पर बढ़ता जल भार, तथा जल आधारित संघर्षों की संभावनाएँ। भूगोल के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन जल संकट की बहुआयामी प्रकृति को स्पष्ट करता है और यह दर्शाता है कि इस संकट का समाधान केवल तकनीकी उपायों से नहीं, बल्कि स्थानिक विशेषताओं, जन सहभागिता, और स्थायित्व आधारित नीतियों से संभव है। इस प्रकार, यह शोधपत्र एक ऐसी समग्र दृष्टि प्रस्तुत करता है, जिसमें जल संकट को केवल संसाधन की समस्या नहीं, बल्कि एक जटिल मानवीय और पारिस्थितिक संकट के रूप में पहचाना गया है, जिसका समाधान एकीकृत, क्षेत्रीय और भूगोल-संवेदनशील योजना द्वारा ही संभव है। 2. अनुसंधान उद्देश्य (Objectives of the Study) 1. भारत में जल संकट के भौगोलिक कारणों की पहचान करना। 2. वर्षा, जल निकासी, भूगर्भीय संरचना और स्थलाकृति जैसे कारकों की भूमिका का विश्लेषण करना। 3. जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत करना। 4. जल प्रबंधन की वर्तमान रणनीतियों की समीक्षा करना। 5. भूगोल आधारित समाधान व नीति सुझाव प्रदान करना। 3. शोध पद्धति (Research Methodology) यह अध्ययन गुणात्मक (qualitative) एवं वर्णनात्मक (descriptive) दोनों विधियों पर आधारित है। इसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्रों, वर्षा प्रतिरूपों, जल स्रोतों, और जल संकट के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। CGWB (Central Ground Water Board), IMD (Indian Meteorological Department), NITI Aayog, और NIWR जैसी संस्थाओं के द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। GIS आधारित मानचित्रण के माध्यम से जल संकट के क्षेत्रीय स्वरूप को रेखांकित किया गया है। 4. भारत में जल संकट की स्थिति भारत में जल संकट एक बहुस्तरीय समस्या के रूप में उभरा है, जो केवल प्राकृतिक कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप, अव्यवस्थित विकास और जल प्रबंधन की विफलताएँ भी शामिल हैं। broadly यह संकट दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (1) भौगोलिक असमानता आधारित संकट: भारत एक भौगोलिक रूप से विविध देश है, जहाँ जल संसाधनों का वितरण असमान है। पूर्वोत्तर भारत — जैसे असम, मेघालय, सिक्किम आदि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 2000–3000 मिमी तक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत — जैसे राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और विदर्भ जैसे क्षेत्र — अल्पवर्षा से पीड़ित हैं, जहाँ यह मात्रा कई बार 200 मिमी से भी कम होती है। इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में नदियाँ ग्लेशियरों से पोषित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूर्णतः मानसून पर निर्भर करते हैं। यह क्षेत्रीय विषमता भारत में जल संकट को और भी जटिल बना देती है। (2) मानवजनित संकट: जल संकट की दूसरी श्रेणी मानवजनित कारकों से उत्पन्न होती है। इनमें प्रमुख हैं: • भूजल का अत्यधिक दोहन: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि के लिए ट्यूबवेल आधारित सिंचाई ने जल स्तर को खतरनाक रूप से नीचे पहुंचा दिया है। • नदियों का प्रदूषण: गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ औद्योगिक, घरेलू और कृषि अपशिष्ट से प्रदूषित हैं। • शहरीकरण और औद्योगीकरण: अनियंत्रित शहरी विस्तार और अपशिष्ट जल की अनुपयुक्त निपटान प्रणाली ने सतही जल स्रोतों को अत्यंत प्रभावित किया है। • वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन: वनस्पति आवरण की हानि जलग्रहण क्षेत्रों को प्रभावित करती है और जल पुनर्भरण की प्रक्रिया बाधित होती है। स्थानिक और कालिक असमानता का प्रभाव: भारत में औसतन 1180 मिमी वार्षिक वर्षा होती है, किंतु इसका लगभग 70% भाग केवल मानसून के दौरान — जून से सितंबर तक — गिरता है। यह वर्षा न केवल सीमित समय के भीतर होती है, बल्कि इसका वितरण भी असमान होता है। एक ही राज्य के भीतर कुछ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो कुछ अल्पवर्षा के शिकार होते हैं। इस विषमता के कारण जल संचयन की स्थायी और समान प्रणाली विकसित करना कठिन हो जाता है। जल की खपत और अपेक्षाएँ: भारत की 80% से अधिक जल आवश्यकता कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाती है, जिसमें पारंपरिक बाढ़ सिंचाई (flood irrigation) जैसी जल अपव्ययी पद्धतियाँ आज भी प्रचलन में हैं। औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में भी जल का उपयोग अत्यधिक बढ़ा है, जिससे घरेलू आपूर्ति पर दबाव और अधिक बढ़ गया है। परिणामस्वरूप: • कई महानगरों (जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली) में Day Zero जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं, जहाँ नलों में जल की आपूर्ति पूर्णतः रुक गई। • ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत सूख चुके हैं और महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से जल लाना पड़ता है। • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सूखा और बाढ़ दोनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे जल संकट और अधिक अनियमित और अस्थिर होता जा रहा है। भारत में जल संकट केवल पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं, बल्कि वितरण, प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के स्तर पर एक समग्र चुनौती है, जिसे यदि भूगोल और पारिस्थितिकी के समन्वित दृष्टिकोण से नहीं सुलझाया गया, तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। 5. प्रमुख जल संकट प्रभावित क्षेत्र भारत का जल संकट राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक है, किंतु कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जो जल संकट से अधिक तीव्र रूप से प्रभावित हैं। ये क्षेत्र विभिन्न कारणों — जैसे अत्यधिक भूजल दोहन, असमान वर्षा वितरण, शुष्क जलवायु, मानसून की विफलता, और जल प्रदूषण — के कारण संकटग्रस्त स्थिति में आ गए हैं। 1. उत्तर भारत (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश): यह क्षेत्र भारत की "हरित क्रांति" का प्रमुख क्षेत्र रहा है, जहाँ गेहूँ और धान जैसी जल-गहन फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ट्यूबवेल आधारित सिंचाई ने भूजल संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया है। • पंजाब के अधिकांश ब्लॉक ‘over-exploited’ श्रेणी में आ चुके हैं। • हरियाणा में भूजल पुनर्भरण की दर बहुत कम है। • पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जल दोहन का स्तर अत्यधिक है, जिससे कई जिलों में जल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है। 2. पश्चिम भारत (राजस्थान, गुजरात): यह क्षेत्र शुष्क और अर्द्ध-शुष्क जलवायु से प्रभावित है। • राजस्थान, भारत का सबसे शुष्क राज्य, जहाँ औसत वर्षा लगभग 250-300 मिमी है, विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों में। • गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में मानसून की अनिश्चितता, अत्यधिक खनन और औद्योगिक उपयोग के कारण जल संकट की स्थिति है। यहाँ पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ जैसे बावड़ियाँ, जोहड़, टांका अब उपेक्षा के शिकार हैं। 3. दक्षिण भारत (तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक): यह क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। यदि मानसून असफल रहता है तो जल संकट गंभीर हो जाता है। • तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहरों में ‘Day Zero’ की स्थिति 2019 में उत्पन्न हो चुकी है। • कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र और तेलंगाना के कई जिले बार-बार सूखे का सामना करते हैं। • कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल संकट की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को दर्शाता है। 4. पूर्वी भारत (झारखंड, ओडिशा): यह क्षेत्र परंपरागत रूप से जल संसाधनों में समृद्ध माना जाता था, किंतु हाल के वर्षों में भूजल स्तर तेजी से गिरा है। • झारखंड में कोयला खनन और औद्योगीकरण ने भूजल पुनर्भरण को बाधित किया है। • ओडिशा के औद्योगिक जिलों जैसे अंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ औद्योगिक अपशिष्ट भी एक बड़ी समस्या बन गए हैं। 5. अन्य संकटग्रस्त क्षेत्र: • बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश): यह क्षेत्र लगातार सूखा प्रभावित रहा है, जहाँ जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियाँ समाप्तप्राय हो चुकी हैं। • मराठवाड़ा (महाराष्ट्र): यहाँ जलग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण और चीनी मिलों के लिए जल की अत्यधिक खपत के कारण हर वर्ष जल संकट विकराल रूप लेता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, भारत के 7,089 अधीनस्थ ब्लॉकों में से 700 से अधिक ब्लॉक ‘जल संकटग्रस्त’ घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से कई को over-exploited, critical और semi-critical श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निष्कर्षतः, भारत के जल संकट को केवल वर्षा या भूगर्भ जल के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि यह एक स्थानिक संकट है, जो हर क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होता है। अतः स्थान-विशेष पर आधारित जल प्रबंधन रणनीतियाँ बनाना अनिवार्य है। 6. भूगोलिक दृष्टिकोण से जल संकट के कारण भारत का जल संकट केवल सामाजिक या प्रशासनिक विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें देश की भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जल संकट के निम्नलिखित भूगोलिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं: 6.1 भौगोलिक विषमता (Geographical Inequality) भारत की भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है, जिससे जल संसाधनों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है। • स्थलाकृति की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी भाग और रेगिस्तान — सभी की जल संसाधन क्षमताएँ भिन्न हैं। • वर्षा वितरण में भारी असमानता है — जहाँ एक ओर मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में प्रतिवर्ष 10,000 मिमी से अधिक वर्षा होती है, वहीं राजस्थान के थार क्षेत्र में औसतन 200 मिमी से भी कम। • तापमान और वाष्पीकरण की दर भी जल संकट को प्रभावित करती है। रेगिस्तानी और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में तापमान अधिक होने से जल का वाष्पीकरण तीव्र होता है, जिससे उपलब्ध जल की मात्रा और अधिक कम हो जाती है। • हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, बर्फ पिघलने पर आधारित सतत प्रवाह बनाए रखती हैं, जबकि दक्कन के पठारी क्षेत्रों की नदियाँ मौसमी हैं। 6.2 जल संसाधनों का असमान वितरण (Uneven Distribution of Water Resources) भारत में कुल उपलब्ध जल संसाधनों का वितरण जनसंख्या और भू-क्षेत्र के अनुपात में संतुलित नहीं है। • गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन देश के कुल जल संसाधनों का लगभग 60% समेटे हुए है, जबकि वहाँ केवल 35–40% जनसंख्या निवास करती है। • दूसरी ओर दक्षिण भारत में कावेरी, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियों पर निर्भर प्रायद्वीपीय क्षेत्र जल की तीव्र कमी का सामना कर रहे हैं, जहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। • पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान और कच्छ क्षेत्र तो अति जलवंचित क्षेत्र बन चुके हैं। 6.3 भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) जल संकट को उत्पन्न करने में भूमि के असंतुलित और अवैज्ञानिक उपयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। • वनों की कटाई से न केवल वाष्पोत्सर्जन और वर्षा में कमी आई है, बल्कि जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण भी हुआ है। • शहरीकरण और कंक्रीटीकरण ने जल पुनर्भरण की परंपरागत प्रक्रिया को बाधित किया है। जल भूमि (wetlands), झीलें और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं। • नदी तटों का अतिक्रमण, मिट्टी कटाव, और जलग्रहण क्षेत्रों में अव्यवस्थित निर्माण कार्य भी जल संकट को बढ़ाते हैं। 6.4 कृषि पर निर्भरता (Monsoon-Dependent Agriculture) भारत की लगभग 60% कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण-पश्चिम मानसून है, जो अनियमित होता जा रहा है। • इस अनिश्चित मानसून पर आधारित कृषि प्रणाली जल संकट की संवेदनशीलता को और अधिक बढ़ा देती है। • पारंपरिक सिंचाई प्रणालियाँ जैसे नाड़ी, जोहड़, बावड़ी आदि की उपेक्षा के कारण आज सिंचाई का पूरा भार ट्यूबवेल और नलकूपों पर है। इससे भूजल का तीव्र शोषण हुआ है। • जल-गहन फसलों जैसे धान और गन्ने की खेती ने भी अनेक क्षेत्रों में जल असंतुलन को जन्म दिया है, विशेषतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सारांशतः, भूगोलिक दृष्टिकोण से जल संकट केवल जल की मात्रा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जल के स्थानिक वितरण, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, प्रबंधन, और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित एक जटिल पारिस्थितिकी-समस्या है। जल संरक्षण के लिए कोई भी नीति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक वह क्षेत्रीय भूगोल और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती। 7. जल संकट के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भारत में जल संकट केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं जो जनजीवन की बुनियादी संरचना को प्रभावित करते हैं। यह संकट ग्रामीण और शहरी, सामाजिक और स्वास्थ्य, तथा आर्थिक उत्पादकता के विभिन्न स्तरों पर गंभीर परिणाम उत्पन्न कर रहा है। 1. ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट और महिलाओं पर प्रभाव: ग्रामीण भारत में पेयजल की उपलब्धता असमान और असंतुलित है। विशेषकर महिलाएँ और किशोरियाँ प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाने में समय और ऊर्जा लगाती हैं। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। • बच्चों की स्कूल उपस्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। • सामाजिक असमानता, विशेषकर दलित बस्तियों में जल स्रोतों तक पहुँच की कठिनाई, और अधिक गहराती है। 2. कृषि उत्पादकता में गिरावट और कृषक आत्महत्याएँ: कृषि भारत की 50% से अधिक जनसंख्या का आजीविका आधार है, और यह पूर्णतः जल पर निर्भर है। जल संकट के कारण: • सिंचाई की अनुपलब्धता से फसलें सूख जाती हैं। • कृषि उत्पादन लागत बढ़ती है। • वर्षा पर निर्भर किसान कर्ज के बोझ में फँस जाते हैं। • विशेषकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और विदर्भ में जल संकट और सूखे के कारण किसान आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 3. स्वास्थ्य पर प्रभाव: जल संकट के कारण अशुद्ध जल का प्रयोग बढ़ता है, जिससे जलजनित रोगों जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस आदि का प्रकोप फैलता है। • ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पेयजल की अनुपलब्धता मातृ और शिशु मृत्यु दर को भी प्रभावित करती है। • शहरी झुग्गी बस्तियों में नालियों का जल पीने योग्य जल से मिल जाने से गंभीर बीमारियाँ फैलती हैं। 4. शहरी जल संकट और सामाजिक असमानता: शहरों में जल वितरण प्रणाली अत्यधिक असमान है: • उच्च वर्गों के पास टैंकर्स और बोतलबंद पानी के विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि झुग्गी बस्तियों में लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। • ‘Day Zero’ की स्थिति (जैसे चेन्नई में 2019) से यह सिद्ध होता है कि शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के दबाव में जल संरचनाएँ टिकाऊ नहीं रह गई हैं। • पानी की निजीकरण प्रक्रिया भी सामाजिक असमानता को और बढ़ाती है। 5. आर्थिक विकास पर प्रभाव: • जल संकट उद्योगों, ऊर्जा उत्पादन और निर्माण क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। • जल-आधारित इकाइयों को स्थानांतरित करना पड़ता है। • उत्पादन लागत बढ़ती है और रोजगार घटता है। इस प्रकार, जल संकट एक बहुआयामी समस्या है, जिसका प्रभाव भारत की सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर रूप से परिलक्षित होता है। इसे केवल संसाधन संकट न मानकर विकास की समग्र चुनौती के रूप में देखना चाहिए। 8. भूगोल आधारित समाधान और उपाय 8.1. वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) जल संकट के निराकरण के लिए स्थानिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल-आधारित उपायों की नितांत आवश्यकता है। यह समाधान स्थानीय भूगोल, वर्षा वितरण, मिट्टी की जलधारण क्षमता, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप होने चाहिए। 8.1. वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting): • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए भवनों की छतों पर जल संचयन प्रणाली अनिवार्य की जानी चाहिए। • दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में यह नीति लागू है, किंतु निगरानी और रखरखाव में लापरवाही है। • पारंपरिक जल संरचनाएँ जैसे बावड़ी, कुंड, सरोवर, आदि का पुनर्जीवन किया जाए, जैसे राजस्थान में जोहर और टांका प्रणाली। 8.2. भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge): • Recharge wells, check dams, soak pits आदि का निर्माण कर वर्षा जल को धरती में समाहित किया जाए। • जलग्रहण क्षेत्र आधारित विकास मॉडल अपनाया जाए। • जल-गहन फसलों की बजाय जैसे धान, गन्ना — कम जल वाली फसलें (ज्वार, बाजरा, दालें) प्रोत्साहित की जाएँ। 8.3. जल साक्षरता और जनजागरूकता: • जल संरक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। • 'Catch the Rain', 'Jal Shakti Abhiyan' जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता के साथ लागू किया जाए। • ‘Water Budgeting’ की अवधारणा ग्रामीण पंचायत स्तर पर लागू की जाए। 8.4. GIS और Remote Sensing तकनीकों का प्रयोग: • जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों की सटीक मैपिंग कर दीर्घकालीन नीति निर्धारण किया जाए। • उपग्रह आधारित निगरानी से झीलों, जलाशयों, भूजल स्तर की नियमित निगरानी की जाए। • जल संसाधनों की data-driven planning से वैज्ञानिक जल प्रबंधन संभव हो सकेगा। 8.5. पारिस्थितिकी आधारित उपाय: • वनों की रक्षा एवं पुनःवनीकरण (Reforestation) से जल चक्र स्थिर होता है। • नदी पुनर्जीवन योजनाएँ जैसे नमामि गंगे को अन्य नदियों पर भी लागू किया जाए। • शहरी जल स्रोतों (तालाब, झील, wetlands) को बचाया जाए। • ‘Eco-sensitive zoning’ को लागू कर जलग्रहण क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए। 9. निष्कर्ष (Conclusion) भारत में जल संकट कोई साधारण संसाधन की कमी नहीं, बल्कि यह एक बहुआयामी और पारिस्थितिकीय रूप से जटिल समस्या है, जिसमें भौगोलिक विषमता, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, कृषि प्रणाली की त्रुटियाँ, और नीति निर्माण में स्थानीय भूगोल की उपेक्षा जैसे अनेक कारक समाहित हैं। इस संकट ने न केवल ग्रामीण जीवन, कृषि और आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मानव विकास सूचकों को भी गहरे रूप से छुआ है। भूगोलिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि एक समान नीति समस्त भारत के लिए कारगर नहीं हो सकती। राजस्थान और तमिलनाडु की जल समस्याएँ पंजाब या असम से भिन्न हैं — अतः क्षेत्रीय जल प्रबंधन रणनीतियाँ जो स्थानीय स्थलाकृति, वर्षा-प्रतिमान, भूजल भंडार और पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखें, अत्यावश्यक हैं। जल एक ऐसा संसाधन है जो न केवल जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी वाहक है। इसलिए, इसका संरक्षण केवल तकनीकी समाधान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामुदायिक भागीदारी, नीति-संवाद, शिक्षा और पारंपरिक जल-संवेदनशील जीवनशैली को भी पुनर्जीवित करना होगा। आज आवश्यकता है कि जल को ‘उपयोग की वस्तु’ नहीं, बल्कि ‘संरक्षण योग्य धरोहर’ के रूप में देखा जाए। जल संकट से निपटने के लिए हमें वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण, सिंचाई दक्षता, पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता और प्रौद्योगिकीय नवाचारों को जन-भागीदारी के साथ जोड़ना होगा। यदि भारत को एक जल-सुरक्षित, जल-साक्षर और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, तो उसे जल नीति को केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। तभी यह बहुआयामी संकट एक अवसर में बदलेगा — ऐसा अवसर जो स्थिरता, समावेशिता और सतत विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकेगा। 10. संदर्भ सूची (References) 1. Central Ground Water Board (CGWB). (2021). Dynamic Ground Water Resources of India (2020). Ministry of Jal Shakti, Government of India. pp. 1–108. 2. NITI Aayog. (2018). Composite Water Management Index – A Tool for Water Management. Government of India. pp. 5–45. 3. Agarwal, A. & Narain, S. (1997). Dying Wisdom: Rise, Fall and Potential of India's Traditional Water Harvesting Systems. Centre for Science and Environment (CSE). pp. 11–89. 4. Singh, R.B. (Ed.). (2015). Water Resources in India: Issues, Concerns and Policy Framework. Springer. pp. 31–70. 5. Mishra, A. (2005). Bharat Mein Jal Sankat: Ek Bhaugolik Sameeksha. Gyanodaya Prakashan, Varanasi. pp. 18–44. 6. Gleick, P.H. (1993). Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water Resources. Oxford University Press. pp. 105–122. 7. Sharma, R.K. (2012). Climate Change and Groundwater Depletion in India. Indian Journal of Geography and Environment, Vol. 11(2), pp. 72–85. 8. United Nations Development Programme (UNDP). (2006). Human Development Report: Beyond Scarcity – Power, Poverty and the Global Water Crisis. pp. 3–27. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-07-04 |
| Cite This | भारत जल-संकटग्रस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से समाधान और उपाय - Ram Singh Jatav - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

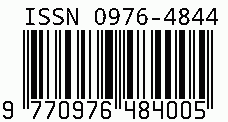
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

