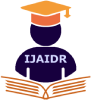
Journal of Advances in Developmental Research
E-ISSN: 0976-4844
•
Impact Factor: 9.71
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Bi-monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 17 Issue 1
2026
Indexing Partners
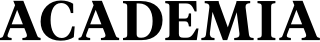













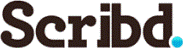




विज्ञान शिक्षण में भारतीय ज्ञान परम्परा का अनुप्रयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
| Author(s) | Prof. ( Dr.) Sunita Jalwania |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कैसे भारतीय ज्ञान परम्परा के सिद्धांत और शिक्षण-प्रथाएँ विज्ञान शिक्षण में प्रभावी रूप से समाविष्ट की जा सकती हैं तथा यह समेकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लक्ष्यों के साथ किस प्रकार अनुकूलन बनाता है। शोध में भारतीय पारंपरिक शिक्षा-परम्पराओं — जैसे गुरु-शिष्य परंपरा, अनुशीलन (शिष्यत्व), पर्यवेक्षणात्मक शिक्षा, स्थानिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ में ज्ञान अर्जन, लोक-ज्ञान तथा समग्र/व्यवहारिक शिक्षण का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही NEP 2020 की प्रमुख धाराओं — जैसे बहु-विषयीता, कौशल-आधारित शिक्षण, व्यावहारिक प्रयोगशाला, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, और शिक्षा में तकनीकी समावेशन के साथ भारतीय ज्ञान परम्परा के तत्त्वों का तालमेल प्रस्तुत किया गया है। अंत में शोध में शिक्षण-नियम, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण-शिल्प तथा नीतिगत सिफारिशें दी गई हैं जो परम्परागत और आधुनिक विधियों का समन्वय कर सकें। प्रस्तावना (Introduction) विज्ञान शिक्षण का इतिहास यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने विज्ञान को मुख्यतः पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिभाषित किया है, जिसमें प्रयोग, विश्लेषण, मापन, और निष्कर्ष को ही वैज्ञानिकता का आधार माना गया। किंतु भारत की प्राचीन परम्परा में विज्ञान को केवल भौतिक या यांत्रिक दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि उसे जीवन की एक समग्र प्रक्रिया के रूप में समझा गया, जहाँ ज्ञान का उद्देश्य मानवता, प्रकृति और ब्रह्मांड के मध्य सामंजस्य स्थापित करना था। इसीलिए भारतीय ज्ञान परम्परा में विज्ञान, दर्शन, कला, भाषा, नैतिकता, तथा आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में शिक्षण केवल विद्यालयों या गुरुकुलों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज और प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास करता था। विज्ञान का शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव और पर्यवेक्षण के माध्यम से होता था, जैसे ऋषियों द्वारा खगोल का निरीक्षण कर ग्रह-नक्षत्रों के गति-चक्र को समझना, किसानों द्वारा मिट्टी और जलवायु के आधार पर फसलों की पहचान करना, या आयुर्वेदाचार्यों द्वारा औषधीय पौधों के गुणों का प्रयोगात्मक अध्ययन करना। इन सभी क्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धति के मूल तत्व— निरीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष और पुनर्परीक्षण — अंतर्निहित थे, यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न रूपों में थी। परंतु उपनिवेशकालीन शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप भारतीय पारंपरिक ज्ञान को “अवैज्ञानिक” या “अप्रासंगिक” मानकर शिक्षा-प्रणाली से अलग कर दिया गया। विज्ञान शिक्षण पश्चिमी संदर्भों और उदाहरणों पर केंद्रित हो गया, जिससे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति एक दूरी और भय की भावना विकसित होने लगी। परिणामस्वरूप विज्ञान एक “अध्ययन विषय” तो बना, किंतु जीवन और समाज से उसका संबंध कमजोर पड़ गया। यही कारण है कि आज आवश्यकता महसूस की जा रही है कि विज्ञान शिक्षण को पुनः भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ा जाए ताकि यह केवल बौद्धिक विकास का नहीं, बल्कि व्यवहारिक और नैतिक विकास का भी माध्यम बन सके। भारतीय ज्ञान परम्परा की विशेषता यह रही है कि वह ज्ञान को स्थिर नहीं मानती, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील और अनुभव-आधारित प्रक्रिया के रूप में देखती है। इस दृष्टि से विज्ञान केवल प्रयोगशाला या कक्षा की सीमा में नहीं, बल्कि पर्यावरण, कृषि, चिकित्सा, खगोल, गणित, तथा दैनिक जीवन के कार्यों में भी निहित है। उदाहरण के रूप में सुष्रुत संहिता में शल्य-क्रिया की विधियों का वर्णन, आर्यभटीय में ग्रहों की गति की गणना, या पिंगलाचार्य की छंदशास्त्र में गणितीय अनुप्रयोग— ये सभी भारतीय परम्परा में विज्ञान की गहराई और मौलिकता को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) इसी समग्र दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का माध्यम न मानकर उसे “जीवन-कौशल” और “समग्र विकास” का साधन बताती है। नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को स्थानीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक संदर्भों के साथ जोड़ना आवश्यक है ताकि शिक्षा अधिक सुलभ, अर्थपूर्ण और प्रभावी बन सके। NEP 2020 का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे जो कि भारतीय ज्ञान परम्परा के मूल उद्देश्य से पूर्णतः मेल खाता है। इस परिप्रेक्ष्य में विज्ञान शिक्षण को केवल तथ्यों और सूत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि खोज, अनुभव और संवाद की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझाया जाए कि विज्ञान का अर्थ केवल आधुनिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वह हमारे खेतों, रसोईघरों, आकाश, नदियों, पर्वतों, और वनस्पतियों में भी विद्यमान है। यदि विज्ञान शिक्षण भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ता है, तो यह विद्यार्थियों के भीतर न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करेगा, बल्कि उनमें प्रकृति, समाज और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित करेगा। इस अध्ययन का यह भी उद्देश्य है कि विज्ञान शिक्षण में पारंपरिक ज्ञान के तत्वों को किस प्रकार समाविष्ट किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी अपने स्थानीय पर्यावरण, सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में विज्ञान को समझ सकें। यह समावेशन न केवल विज्ञान शिक्षा को सजीव और प्रासंगिक बनाएगा, बल्कि यह विद्यार्थियों में आत्मगौरव, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। अंततः, भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के मध्य कोई विरोध नहीं, बल्कि गहरा संबंध है। जहाँ पश्चिमी विज्ञान ने प्रयोग और मापन को महत्व दिया, वहीं भारतीय परम्परा ने अनुभव और चेतना के समन्वय को। जब ये दोनों दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक बनकर विज्ञान शिक्षण में लागू होंगे, तब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव होगा जो न केवल बौद्धिक रूप से समृद्ध बल्कि सांस्कृतिक रूप से सशक्त और नैतिक रूप से जागरूक नागरिकों को तैयार करेगी। समस्यावली और अध्ययन का उद्देश्य (Problem Statement & Objectives) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विज्ञान शिक्षा के कई ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक विमर्शों का समुचित समन्वय न होना देखा गया है। विद्यार्थी विज्ञान को कभी-कभी केवल करियर-उन्मुख या पठनीय विषय मानते हैं, जबकि उसकी व्यवहारिक उपयोगिता और स्थानीय समस्याओं से जुड़ाव कम होता है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. भारतीय ज्ञान परम्परा के ऐसे तत्वों की पहचान करना जो विज्ञान शिक्षण के साथ तालमेल कर सकते हैं। 2. NEP 2020 के प्रावधानों के संदर्भ में उन तत्वों का शैक्षिक प्रयोग और नीति-संदर्भ तैयार करना। 3. शिक्षण-पद्धतियों, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन में समावेशन हेतु व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तावित करना। सैद्धान्तिक पृष्टभूमि (Theoretical Background) भारतीय ज्ञान परम्परा का मूल आधार यह रहा है कि ज्ञान केवल तर्क या बुद्धि का उत्पाद नहीं, बल्कि अनुभव, अवलोकन, अंतःप्रेरणा, और व्यवहार का समन्वय है। भारत के वैदिक, उपनिषदिक और दार्शनिक ग्रंथों में ज्ञान को "सत्य की खोज" और "जीवन का समग्र अनुभव" कहा गया है। “साऽ विद्या या विमुक्तये” — अर्थात वह विद्या जो जीवन को मुक्ति की ओर ले जाए। इस दृष्टिकोण में शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मानव जीवन को सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत करना है। यही दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परम्परा की सैद्धान्तिक नींव बनाता है। इस परम्परा में ज्ञान का स्वरूप बहु-आयामी (multi-dimensional) है। यह केवल सिद्धान्त नहीं, बल्कि व्यवहार और प्रयोग से जुड़ा हुआ है। भारतीय ग्रंथों में चार प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है । श्रुति (सुनी हुई विद्या), स्मृति (अनुभव और परंपरा से प्राप्त ज्ञान), प्रत्यक्षा (प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान) और अनुमान (तार्किक निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान)। ये सभी मिलकर भारतीय ज्ञान प्रणाली को एक समग्र और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी कारण भारतीय परम्परा में गणित, खगोलशास्त्र, कृषि, चिकित्सा, रसायन, धातु-विज्ञान, और वास्तु जैसे विषय केवल आस्था या प्रतीक नहीं रहे, बल्कि गहन अनुभवजन्य अध्ययन का परिणाम रहे हैं। गुरु-शिष्य परंपरा इस ज्ञान-प्रणाली का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक रही है। इसमें शिक्षा को एक संवादात्मक और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया, जहाँ गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक होता था। यह प्रणाली शिक्षार्थी की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि और गति को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक अनुशीलन पर बल देती थी। आधुनिक शिक्षाशास्त्र में यह दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज़्म (Constructivism) के सिद्धांत से मेल खाता है, जहाँ विद्यार्थी स्वयं अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। भारतीय लोक-ज्ञान और पारंपरिक तकनीकें भी इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक विस्तार हैं। कृषि, चिकित्सा, जल-संरक्षण, निर्माण, वस्त्र-निर्माण, तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में लोक समुदायों ने अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक विधियाँ विकसित कीं। जैसे राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ (बावड़ी, जोहड़, तालाब, टांका आदि) जल प्रबंधन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत के किसान मौसमी परिवर्तन का अनुमान पौधों, पशुओं और वायुमंडलीय संकेतों से लगाते हैं । यह उनके स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान का परिणाम है। ये सभी उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज ने विज्ञान को हमेशा व्यवहार और जीवन से जोड़कर देखा। इन पारंपरिक दृष्टिकोणों की सैद्धान्तिक जड़ें आधुनिक शिक्षण सिद्धांतों से भी गहराई से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए: • अन्वेषणात्मक शिक्षण (Inquiry-based Learning): यह विधि विद्यार्थियों में जिज्ञासा और प्रयोग की भावना को बढ़ावा देती है। भारतीय गुरुकुल प्रणाली में प्रश्न पूछने की परंपरा को बहुत महत्व दिया गया — “कथं, किमर्थं, कुतः” (क्यों, कैसे, किससे) जैसे प्रश्नों के माध्यम से शिष्य ज्ञान का सृजन करते थे। • अनुभवात्मक शिक्षण (Experiential Learning): यह सिद्धांत कहता है कि सीखना तभी स्थायी होता है जब वह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो। भारतीय परम्परा में शिक्षा पुस्तकीय न होकर अनुभव-आधारित थी — चाहे वह योगाभ्यास हो, धातु-निर्माण, औषधि-संग्रहण या गणना की विधियाँ। • समग्र शिक्षण (Holistic Education): आधुनिक शिक्षा मनुष्य के केवल बौद्धिक विकास पर केंद्रित हो गई है, जबकि भारतीय परम्परा में शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी का संतुलित विकास करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) इसी समग्र दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करती है। यह नीति शिक्षा को केवल नौकरी-केंद्रित या विषयगत नहीं, बल्कि बहुआयामी, कौशल-आधारित और मूल्यपरक बनाने की बात करती है। NEP के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में “21वीं सदी के कौशल” जैसे आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और नैतिक चेतना का विकास करना है। यह नीति स्थानीय भाषा में शिक्षा, अंतःविषयक शिक्षण, परियोजना-आधारित शिक्षण, और अनुभवात्मक शिक्षण पर विशेष बल देती है — जो सभी भारतीय पारंपरिक शिक्षण मूल्यों से गहराई से जुड़ते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान परम्परा और NEP 2020 के बीच कोई विरोध नहीं, बल्कि पूरक संबंध विद्यमान है। भारतीय परम्परा जहाँ अनुभव, अंतर्ज्ञान और नैतिकता पर आधारित शिक्षा की वकालत करती है, वहीं NEP 2020 इन मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। उदाहरणतः — • गुरु-शिष्य परंपरा का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मॉडल, NEP के मेंटरिंग सिस्टम के अनुरूप है। • पारंपरिक शिक्षा का समुदाय-आधारित ज्ञान-संवर्धन, NEP के स्कूल-कम्युनिटी इंटरैक्शन मॉडल से मेल खाता है। • लोक-ज्ञान और पारंपरिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दृष्टिकोण, NEP के कौशल-आधारित शिक्षा के सिद्धांतों को मज़बूत करता है। इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप से देखा जाए तो भारतीय ज्ञान-परम्परा और NEP 2020 दोनों का साझा लक्ष्य है । शिक्षा को जीवन, समाज और पर्यावरण से जोड़ना। यदि विज्ञान शिक्षण में इन दोनों की समेकित दृष्टि को अपनाया जाए, तो विद्यार्थी न केवल वैज्ञानिक रूप से दक्ष बनेंगे बल्कि नैतिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। यह समेकन भारत को उस दिशा में अग्रसर करेगा जहाँ आधुनिक वैज्ञानिकता और पारंपरिक ज्ञान एक-दूसरे के पूरक बनकर “आधुनिक भारत” की नींव को सुदृढ़ करेंगे। साहित्य समीक्षा (Literature Review) अनेक अध्ययनों ने यह संकेत किया है कि स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान का समावेश शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि और सीखने की गहराई बढ़ाता है। वैकल्पिक स्कूल प्रणालियों और कुछ शोधों में पारंपरिक कृषि ज्ञान को विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल करने से सिद्धान्तों की समझ और स्थानीय सन्दर्भ में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि मिली। गुरु-शिष्य परम्पराओं की शिक्षण-शैली में संवादात्मक, ऑब्ज़र्वेशन-आधारित और प्रयोगात्मक अध्ययन शामिल होते हैं, जो आधुनिक शिक्षा-श्रेणियों में भी प्रभावी सिद्ध होते हैं। NEP 2020 पर लिखी कई नीतिगत-विश्लेषणात्मक कृतियों में यह सुझाया गया है कि नीति की व्यावहारिकता तभी सफल होगी जब उसे स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, स्थानिक शिक्षक प्रशिक्षण तथा सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू किया जाए। यद्यपि बहु-लेखों ने पारंपरिक ज्ञान के लाभों का समर्थन किया है, किंतु चुनौतियाँ—जैसे ज्ञान का वैधानिक सत्यापन, मिथक और विज्ञान के बीच भेद, तथा पाठ्यक्रम में सीमित समय—भी उद्धृत हुए हैं। इस संदर्भ में आवश्यक है कि पारंपरिक ज्ञान के तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जाँचा जाए और शैक्षिक रूप में उसे अनुकूलित किया जाए। वर्तमान वर्ष 2025 में शोध का झुकाव भारतीय ज्ञान परम्परा और शैक्षणिक नवोन्मेष (educational innovation) के संगम की ओर देखा जा रहा है। “Bridging Tradition and Innovation: The Role of Indian Knowledge Systems in Reimagining Education Today for Gen Z Learners” (RSIS International) शीर्षक शोध में यह दर्शाया गया है कि कैसे IKS आधुनिक पीढ़ी (Gen Z) के शिक्षार्थियों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और अनुभव-आधारित शिक्षण शैली के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इसी दिशा में “The Importance of Indian Knowledge Systems (IKS) for Undergraduate Students” (Science Publishing Group) नामक लेख ने उच्च शिक्षा के स्तर पर IKS के समावेश की आवश्यकता और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर बल दिया है। इन अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया कि अब भारतीय ज्ञान परम्परा को केवल प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा तक सीमित न रखकर, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के स्तर पर भी समाहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2024 में IKS के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसके आधुनिक विज्ञान-शिक्षण में योगदान पर कुछ उल्लेखनीय शोध प्रकाशित हुए। “A Study of the Scientific Approach Inherited in the Indian Knowledge System (IKS)” (scientifictemper.com) नामक अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया कि भारतीय परम्परा में वैज्ञानिक अन्वेषण (scientific inquiry) के तत्व — जैसे अवलोकन, प्रयोग और अनुभव — प्राचीन काल से ही विद्यमान रहे हैं। यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि इन तत्त्वों को वर्तमान विज्ञान-शिक्षा में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के प्रभाव, उद्देश्यों और व्यावहारिक कार्यान्वयन पर गहन विचार-विमर्श हुआ। “National Education Policy of India: A Comprehensive Roadmap for Transformative Education” (HM Journals) नामक लेख में नीति की प्रमुख विशेषताओं — जैसे कौशल-विकास, व्यावसायिकता, समग्र शिक्षा और अंतःविषय (interdisciplinary) दृष्टिकोण — का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2022 में COVID-19 महामारी के पश्चात शिक्षा-व्यवस्था में आए डिजिटल परिवर्तन और व्यवहारिक शिक्षण की चुनौतियों ने विज्ञान-शिक्षण को नई दिशा दी। इस संदर्भ में “Response to the COVID-19 Pandemic: Physics Teaching in India” (arXiv.org) शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें महामारी के दौरान भौतिक विज्ञान के शिक्षण में उत्पन्न अवरोधों और डिजिटल विभाजन की समस्याओं का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन ने यह भी इंगित किया कि परिस्थितियों के कारण शिक्षक पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों को पुनः मूल्यांकित करने लगे। वर्ष 2021 में भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) और विज्ञान-शिक्षण के प्रत्यक्ष समन्वय पर बहुत अधिक संगठित शोध उपलब्ध नहीं थे, तथापि इस अवधि में IKS को शिक्षा के क्षेत्र में समाहित करने और स्थानीय ज्ञान-प्रथाओं की उपयोगिता पर कुछ प्रारंभिक प्रयास अवश्य दिखाई दिए। उदाहरण स्वरूप, “Implementation of IKS-based Curricula in Schools: An Empirical Study” (apu.res.in) नामक शोध में विद्यालय स्तर पर भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित पाठ्यक्रमों के प्रयोगात्मक अनुप्रयोग का अध्ययन किया गया। इस प्रकार, यद्यपि इस वर्ष अनुसंधान सीमित था, तथापि यह प्रवृत्ति स्पष्ट होने लगी कि शिक्षाविद और शोधकर्ता पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के संयोजन की प्रासंगिकता को गंभीरता से समझने लगे थे। यह कालांश भविष्य के समन्वयात्मक अनुसंधानों के लिए एक आधारभूमि तैयार करता है। अनुसंधान पद्धति (Methodology) यह शोध साहित्य-आधारित विश्लेषणात्मक (descriptive-analytical) अध्ययन है, जिसमें प्राथमिक सूचना के स्थान पर द्वितीयक स्रोतों—शैक्षिक नीतियाँ, शोध-पत्र, प्रायोगिक केस-स्टडीज, और पारंपरिक ज्ञान-समूहों पर प्रकाशित मेटा-विश्लेषण—का उपयोग किया गया है। साथ ही कुछ प्रायोगिक अनुशंसाएँ और उदाहरणात्मक शिक्षण-योजनाएँ तैयार की गई हैं जो फील्ड-स्थिति में प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं। अध्ययन में निम्नलिखित चरण अपनाए गए: (1) भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रमुख तत्त्वों का वर्गीकरण, (2) NEP 2020 के प्रावधानों का विश्लेषण, (3) दोनों के समन्वय के व्यवहारिक मोडलों का प्रस्ताव, तथा (4) पाठ्यक्रम/शिक्षण दृष्टिकोणों के लिए सिफारिशें। भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रमुख तत्त्व और उनका विज्ञान शिक्षण में उपयोग 1. अनुभवात्मक (Empirical) ज्ञान और पर्यवेक्षण बहुत से पारंपरिक ज्ञान-श्रृंखलाएँ अनुभव और अवलोकन (observation) पर आधारित हैं, जैसे मौसम चक्रों का अनुमान, जल-संग्रहण के स्थानीय तरीके, मिट्टी की प्रकार-नियतियाँ इत्यादि। विज्ञान शिक्षण में इन्हें प्रयोगशाला और फील्ड-कार्य के माध्यम से जोड़कर विद्यार्थियों को निरीक्षण-प्रेरित शिक्षण दिया जा सकता है। उदाहरण: स्थानीय फसल-चक्र का अध्ययन करके जीवविज्ञान एवं पारिस्थितिकी के सिद्धान्तों को समझाना। 2. अंतःविषयता (Interdisciplinarity) भारतीय परम्परा में ज्ञान सामान्यत: विभाजित नहीं था। खगोलशास्त्र से गणित, आयुर्वेद से रसायनशास्त्र तक गहरा अंतर्धान रहता था। NEP 2020 भी अंतःविषयक शिक्षा पर जोर देता है। स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रमों में इतिहास, भाषा, कला और स्थानीय हस्तशिल्प के साथ विज्ञान के प्रोजेक्ट जोड़े जा सकते हैं — उदाहरण: पारंपरिक कुम्हारियों की तकनीक को भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों के साथ जोड़ना। 3. स्थानीय भाषा और संदर्भ में शिक्षण गुरु-शिष्य परम्परा और लोक-ज्ञान स्थानीय भाषाओं में संरक्षित रहा है। विज्ञान के जटिल सिद्धान्तों को स्थानीय भाषा में और स्थल-विशिष्ट उदाहरणों के साथ पढ़ाने से समझ में वृद्धि होती है और भाषा-आधारित बाधाएँ घटती हैं। NEP 2020 का बहु-भाषी शिक्षण दृष्टिकोण इसी तर्क का समर्थन करता है। 4. नैतिक और आदर्शगत शिक्षा (Ethical & Holistic Education) भारतीय शिक्षा-परम्परा में न केवल तर्क बल्कि जीवन-धार्मिक और नैतिक शिक्षाएँ भी शामिल रहती थीं। विज्ञान शिक्षण में जिम्मेदार प्रयोगशाला-अभ्यास, पर्यावरणीय नैतिकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जिम्मेदारी जोड़कर विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। 5. प्रायोगिक कला और हस्तशिल्प के माध्यम से सिद्धान्तों की समझ पारंपरिक हस्तशिल्पों में उपयोग किए गए भौतिक सिद्धान्त और रासायनिक प्रक्रियाएँ विज्ञान कक्षा में प्रयोग के रूप में उपयोगी हो सकती हैं। उदाहरण: कुम्हार के बर्तन बनाते समय घर्षण, धारकता, जल-आवेश और थर्मल गुणों का अध्ययन। NEP 2020 के प्रावधान और पारम्परिक ज्ञान का समन्वय NEP 2020 ने शिक्षा को समग्र, बहु-विषयी और प्रयोगात्मक बनाने का स्पष्ट उदेश्य रखा है। इसके प्रमुख प्रावधान जैसे स्कूल शिक्षा का पुनर्गठन (5+3+3+4), बहुभाषिकता, कौशल-आधारित पाठ्यक्रम, प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण, स्कूल-समुदाय भागीदारी, तथा शिक्षक प्रशिक्षण—ये सभी पारम्परिक ज्ञान की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप: • प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण (PBL): विद्यार्थी समुदाय आधारित समस्याओं पर परियोजनाएँ कर सकते हैं — जैसे स्थानीय जल-स्रोत संरक्षण पर शोध, पारंपरिक कृषि विधि का वैज्ञानिक मूल्यांकन आदि। इसके माध्यम से परम्परागत ज्ञान की सत्यता और आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण का मेल होता है। • माध्यमिक भाषा में शिक्षा: स्थानिक भाषाओं में विज्ञान की अवधारणाओं को सिखाने से अवधारणा-गत समझ बेहतर होती है और पारम्परिक शब्दावली का संरक्षण भी सम्भव होता है। • शिक्षक प्रशिक्षण: NEP के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षण (Continuous Professional Development) में पारम्परिक ज्ञान-श्रोताओं और स्थानीय विशेषज्ञों को सम्मिलित कर, शिक्षकों को स्थानिक ज्ञान को विज्ञान पाठ्यक्रम में अनुकूलित करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। व्यवहारिक मॉडल और पाठ्यक्रम संकल्पनाएँ (Practical Models & Curriculum Ideas) 1. स्थानीय-ज्ञान आधारित विज्ञान यूनिट: प्रत्येक विज्ञान इकाई (जैसे ऊर्जा, पानी, मिट्टी) को स्थानीय परियोजना के साथ जोड़ें — विद्यार्थियों को स्थानीय कृषक, कुम्हार, आयुर्वेदिक चिकित्सक आदि से संवाद कराकर परियोजना-रिपोर्ट तैयार कराना। 2. इन्टर्न-शिप/फील्ड-रोटेशन: जूनियर स्तर पर स्कूल—समुदाय साझेदारी के जरिये छोटे-फील्ड-इंटर्नशिप का आयोजन, जहाँ विद्यार्थी पारंपरिक तकनीकों का अवलोकन करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। 3. पाठ्यपुस्तक में केस-स्टडी समावेशन: पारंपरिक तकनीकों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित केस-स्टडीज़ को पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया जाए। 4. मल्टीमीडिया एवं स्थानीय भाषा श्रोत: वीडियो, ऑडियो और स्थानीय ग्रंथों का उपयोग कर पारंपरिक ज्ञान की मौखिक परम्पराओं को रिकॉर्ड कर के शिक्षण में उपयोग करें। 5. मूल्यांकन सुधार: परीक्षाओं में सिर्फ स्मृति-निरपेक्ष प्रश्नों के बजाए प्रोजेक्ट-रिपोर्ट, फील्ड-डायरी, प्रस्तुति और मौखिक परिक्षण पर भी वजन दें ताकि पारम्परिक ज्ञान का उपयोग और व्यावहारिक समझ का सही आकलन हो। चुनौती एवं सीमाएँ (Challenges and Limitations) भारतीय ज्ञान परम्परा को विज्ञान शिक्षण में समेकित करने में कुछ व्यावहारिक और दार्शनिक चुनौतियाँ उपस्थित होंगी: • वैज्ञानिक मान्यता और मिथक का पृथकीकरण: पारंपरिक ज्ञान में कई उपयोगी विधियाँ हैं पर कुछ मिथकीय मान्यताएँ भी हो सकती हैं — इन्हें वैज्ञानिक पद्धति से जाँचना आवश्यक है। • पाठ्यक्रम भार और समय: सीमित विद्यालयीय समय में नए तत्वों का समावेश पाठ्यक्रम को भारी कर सकता है; अतः समेकन के लिए पुनर्गठित और प्राथमिकतायुक्त पाठ्यक्रम आवश्यक है। • शिक्षक क्षमता: स्थानीय ज्ञान का प्रयोग तभी प्रभावी होगा जब शिक्षक उसे समझते और सिखा सकते हों — इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक विशेषज्ञों का समावेश अनिवार्य है। • स्रोत और प्रमाणन: पारंपरिक ज्ञान के प्रमाणित स्रोतों का संकलन और स्थानीय विशेषज्ञों के वैधानिक भागीदारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। नीति सिफारिशें (Policy Recommendations) 1. पाठ्यक्रम में लचीला मॉड्यूल: केंद्रीय और राज्य स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐसे लचीले मॉड्यूल निर्धारित किए जाएँ जो स्थानीय ज्ञान पर आधारित परियोजनाओं को सम्मिलित करने की अनुमति दें। 2. शिक्षक-पेशेवर विकास: NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पारंपरिक ज्ञान, समुदाय-सहयोग और फील्ड-प्रोजेक्ट डिज़ाइन के प्रशिक्षण शामिल किए जाएँ। 3. स्थानीय विशेषज्ञों का समावेश: स्कूलों में 'समुदाय विशेषज्ञ-खण्ड' बनाया जाए जहाँ पारंपरिक जानकारों को अतिथि-शिक्षक/परामर्शदाता के रूप में आमंत्रित किया जाए। 4. वैज्ञानिक जाँच एवं प्रमाणन: पारंपरिक विधियों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए और जिन विधियों की वैज्ञानिक वैधता प्रमाणित हो, उन्हें विस्तृत पाठ्यक्रमीकृत मॉड्यूल के रूप में शामिल किया जाए। 5. मल्टी-लैंग्वेज स्रोत और डिजिटल आर्काइव: स्थानीय भाषाओं में पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल संग्रह बनाकर उसे शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सुलभ कराया जाए। निष्कर्ष (Conclusion) विज्ञान शिक्षण में भारतीय ज्ञान परम्परा का समायोजन केवल सांस्कृतिक पुनर्स्मरण या परम्परा के संरक्षण का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक सार्थक शैक्षणिक पुनर्परिभाषा है, जो आधुनिक विज्ञान को स्थानीय अनुभवों, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टियों और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाती है। भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) में विद्यमान वैज्ञानिक चेतना — जैसे अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण, तथा सतत चिंतन — आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के साथ गहरे रूप से संगत हैं। अतः इन दोनों के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण संभव है जो न केवल ज्ञान-संचयन पर, बल्कि ज्ञान-सृजन, अनुप्रयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी आधारित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक दूरदर्शी दस्तावेज़ सिद्ध होती है। यह शिक्षा को केवल तथ्यों के संग्रहण तक सीमित न रखकर उसे एक समग्र मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में देखती है। नीति का यह आग्रह, कि शिक्षा बहुभाषी, बहु-विषयक, और अनुभव-आधारित हो। भारतीय ज्ञान परम्परा की आत्मा से स्वाभाविक रूप से मेल खाता है। NEP 2020 में स्थानीय ज्ञान, मातृभाषा, और पारंपरिक शिल्प-प्रणालियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो अनुशंसा की गई है, वह विज्ञान शिक्षण को भी स्थानीय संदर्भों से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यदि नीति-निर्माता, शिक्षक, शोधकर्ता और समुदाय एक साझा दृष्टि के साथ कार्य करें — तो विज्ञान शिक्षण को केवल प्रयोगशाला और पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रखकर, जीवन और समाज से जुड़ा हुआ शिक्षण-अनुभव बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में IKS के वैज्ञानिक आयामों को सम्मिलित किया जाए, स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, और विद्यार्थियों को अपने परिवेश में विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान के स्रोतों से परिचित कराया जाए। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परम्परा का विज्ञान शिक्षण में समावेश शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, संदर्भ-संवेदनशील और सृजनशील बना सकता है। यह न केवल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच (critical thinking) और समस्या-समाधान (problem-solving) की क्षमताएँ विकसित करेगा, बल्कि उनमें पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का भी संचार करेगा। अंततः, यह कहा जा सकता है कि विज्ञान शिक्षण में भारतीय ज्ञान परम्परा का प्रयोग केवल अतीत की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि भविष्य की पुनर्रचना का एक सशक्त माध्यम है। जब विज्ञान आधुनिकता के साथ परम्परा का संतुलन साधेगा, तब शिक्षा केवल “जानने” की प्रक्रिया नहीं रहेगी — वह “समझने, अनुभव करने और सृजन करने” की प्रक्रिया बन जाएगी। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है और यही NEP 2020 की आत्मा भी। संदर्भ (References) I. Books and Monographs 1. Agrawal, D. P. (2009). Indian Science and Technology in the Eighteenth Century. New Delhi: Oxford University Press. 2. Achar, R. (2017). Indian Knowledge Systems: Their Relevance for Modern Education. Delhi: Aryan Books International. 3. Basu, A. (2018). Education and the Indian Tradition of Learning. New Delhi: Sage Publications. 4. Bharadwaj, S. (2021). Integrating Traditional Knowledge in Modern Science Education. Jaipur: Rawat Publications. 5. Chatterjee, S. (2019). The Philosophy of Indian Science. Kolkata: University of Calcutta Press. 6. Goel, A., & Mishra, P. (2020). Indian Knowledge Systems and Education Reforms. New Delhi: Concept Publishing Company. 7. Kumar, R. (2022). Science Teaching in Indian Context: Challenges and Opportunities. New Delhi: NCERT. 8. Raina, D. (2019). The Making of Modern Indian Science. Delhi: Permanent Black. 9. Sharma, M. (2023). Bharatiya Gyan Parampara aur Adhunik Shiksha. Varanasi: Vishwavidyalaya Prakashan. 10. Subrahmanyam, K. (2018). Scientific Temper and Indian Thought. Hyderabad: Orient Blackswan. II. Journal Articles (National & International) 11. Anand, S. (2022). “Reinterpreting Science Pedagogy through Indigenous Knowledge Systems.” Journal of Indian Education, 48(3), 42–57. 12. Banerjee, R. (2021). “Science Education and the NEP 2020: A Framework for Integration.” Educational Review India, 59(2), 88–101. 13. Bhattacharya, T. (2020). “Indian Knowledge Systems and the Pedagogical Shift in NEP 2020.” University News, 58(33), 12–17. 14. Gupta, N., & Sinha, R. (2023). “Bridging Modern Science with Traditional Wisdom: An Indian Perspective.” International Journal of Education and Research, 11(1), 1–13. 15. Joshi, V. (2021). “Science Education in India: From Colonial Legacy to NEP 2020.” Indian Journal of Education Studies, 45(4), 67–81. 16. Kaur, P. (2024). “Reviving Indigenous Knowledge for STEM Education.” Asian Education Review, 12(1), 23–36. 17. Mahajan, S. (2023). “Value-based Science Education in the Light of NEP 2020.” Journal of Educational Research and Innovation, 10(2), 55–69. 18. Nair, R. (2022). “Integrating Local Wisdom with Global Science: Lessons from Indian Knowledge Systems.” Education and Society, 44(1), 75–92. 19. Pandey, A. (2020). “Reconceptualizing Science Teaching: An Indian Knowledge Approach.” Contemporary Education Dialogue, 17(3), 115–129. 20. Singh, S. K. (2025). “NEP 2020 and the Future of Science Pedagogy in India.” Indian Journal of Pedagogical Studies, 62(1), 101–118. III. Government Reports and Official Documents 21. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Ministry of Education. 22. NCERT. (2022). National Curriculum Framework for School Education. New Delhi: NCERT. 23. NITI Aayog. (2021). Strategy for Integrating Traditional Knowledge Systems in Education. New Delhi: Government of India. 24. Ministry of Education. (2023). Annual Report on Science and Education Integration. New Delhi. 25. UGC. (2022). Guidelines for Indian Knowledge Systems (IKS) in Higher Education Institutions. New Delhi. 26. AICTE. (2021). Handbook on Indian Knowledge Systems (IKS) for Engineering and Science Education. New Delhi: AICTE-IKS Division. 27. NCERT. (2021). Position Paper on Science Education and IKS Integration. New Delhi. 28. CBSE. (2024). Incorporation of Indian Knowledge in Science Curriculum. New Delhi: Central Board of Secondary Education. IV. International Organization Reports 29. UNESCO. (2021). Indigenous Knowledge and the Future of Education. Paris: UNESCO Publishing. 30. UNESCO. (2023). Reimagining Science Education for Sustainable Development. Paris. 31. World Bank. (2022). Education for Knowledge Societies in South Asia. Washington, DC. 32. OECD. (2020). Transforming Education through Local Knowledge Integration. Paris. 33. UNDP. (2023). Indigenous Knowledge Systems and Sustainable Education Models. New York: UNDP. V. Theses, Dissertations, and Research Projects 34. Meena, R. (2022). A Study of Indian Knowledge Systems in Modern Science Curriculum. Ph.D. Thesis, University of Rajasthan. 35. Iyer, P. (2021). Relevance of Ancient Indian Science in Contemporary Education. Ph.D. Dissertation, Banaras Hindu University. 36. Khan, A. (2023). NEP 2020 and the Pedagogical Transition in Science Education. M.Ed. Dissertation, Jamia Millia Islamia. 37. Joshi, L. (2024). Pedagogical Innovations through Integration of IKS in Science Teaching. Ph.D. Thesis, Delhi University. VI. Online Sources and Websites 38. Indian Knowledge Systems (IKS) Division, Ministry of Education. (2025). Retrieved from https://iksindia.org 39. NCERT Digital Repository. (2024). “Integrating Traditional Knowledge in Science Teaching.” Retrieved from https://ncert.nic.in 40. AICTE IKS Portal. (2023). “Indian Knowledge Systems and Scientific Learning.” Retrieved from https://aicte-india.org/iks 41. Ministry of Education. (2022). “Implementation Framework for NEP 2020.” Retrieved from https://education.gov.in 42. CBSE Academic Repository. (2024). “Inclusion of Local Knowledge in Science Curriculum.” Retrieved from https://cbseacademic.nic.in 43. Press Information Bureau. (2023). “Government Initiative to Promote Indian Knowledge Systems.” Retrieved from https://pib.gov.in VII. Conference Papers and Seminars 44. Sharma, R. (2022). “Pedagogical Strategies for Integrating IKS in Science Teaching.” Proceedings of the National Conference on Innovative Education, Jaipur, India. 45. Verma, S., & Gupta, N. (2023). “The Role of NEP 2020 in Mainstreaming Indian Knowledge Systems.” Proceedings of International Conference on Reimagining Education, New Delhi. |
| Keywords | . |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 16, Issue 2, July-December 2025 |
| Published On | 2025-11-12 |
| Cite This | विज्ञान शिक्षण में भारतीय ज्ञान परम्परा का अनुप्रयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - Prof. ( Dr.) Sunita Jalwania - IJAIDR Volume 16, Issue 2, July-December 2025. |
Share this

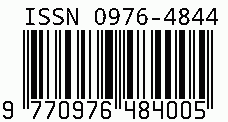
CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJAIDR DOI prefix is
10.71097/IJAIDR
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.

